एक ऐसी छवि जो बाज़ार में तो कभी गलियों में घुमक़्कड़ों की तरह जिंदगी के रंगों को जीते हैं और हमारे आस-पास भी ऐसे कई शख्स हैं जो हमें बहुत से नुक्कड़, चौराहों और गलियों में गाना गाते, अपने आपसे बातें करते, चीखते-चिल्लाते और उन बच्चों को गालियाँ बकते नज़र आते हैं - जो उन्हें पागल-पागल कहकर चिड़ाते हैं।
न वो ये साबित कर सकते हैं कि वो पागल नहीं हैं और न वो कहते की जुबान रोक सकते हैं वो बस उनसे दूर अपने आपको कहीं समेटना चाहते हैं, कहीं किसी कोने में। जो कौना समाज उन्हे नहीं देता और अगर देता भी है तो एक चुप्पी के साथ... जिसमें न उनको सुनने वाले कान होते हैं और न ही बत से बत्तर हालात में देखने वाली आँखें, न रहने को छत और न पहन्ने को साफ कपड़े, कोइ ढ़ैर सारे लिहाफ-बिसतरों मे लिपटा दिखाई पड़ता है, मौसम चाहे कैसा भी हो उसे न गर्मी लगती है और न सर्दी...
तो कोई सिर्फ़ चार पट्टीयों मे लिपटा सड़को पर घूमता रहता है।
उसके लिए न शर्म है और न लोगों के ताने कि "तूने पहन क्या रखा है?"
और अपने नंगे शरीर को पूरे बाज़ार में लिए फिरता है न कोई उसको दो कपड़े पहनाने वाला है और न कोई ये कहने वाला कि "दो कपड़े तो पहन ले"
कोई-कोई तो इस कदर चीख़ता हुआ दिखता है कि मानो उसको कोई सरे-आम सड़क पर हंटरों से मार रहा हो पर उसको मारने वाला कोइ नहीं होता वो अपने आप उस चोट को महसूस करता और जोर-जोर से चिल्लाता, अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालता, न जाने वो जोर और वो कड़कपन उसकी आवाज़ में कहां से आता है?
कुछ ही दिन पहले की बात है एक शख्स दिल्ली गैट से पहले पड़ने वाले तिराहे चौक के एक साइड में बैठा अपने आप में बड़बड़ा सा रहा था। मैं उसे देख वहीं एक जनरल स्टोर पर रुक गया और कुछ खरीदने लगा। बार-बार मेरी नज़रें उसे देखने और मेरे कान उसे सुनने को बेचेन से हो गए थे। दुकानदार ने पूछा भी कि ....
क्या लेना है ?
मेरी नज़रें एक पल उसकी तरफ मुड़ी और वापस उसको देखने लगी और होटों से आवाज़ निकली " ब्लू पेन देदो कोई सा " अपने हाथों को कान पर लगाए मोबाइल की कल्पना ने उसे अंधा बना दिया था कि उसके पास मोबाइल है।
मैं उसे ही देख रहा था।
वो : " हैलो हां मजिस्टेड साहब हां मेरी कल की फ्लाइट है, मैं कल नहीं आ सकता "...
" हाँ हाँ वो मैं अभी एक जरूरी मीटींग में हुँ मैं कल आउंगा "...
" हैलो शुकला साहब मेरी अमेरीका का टीकट कटवा दो, मैं कल आपसे मिलनें आउंगा "...
ऐसी कई सारी बातों से वो अपने आपको एक रहीस आदमी की छवि में उतारता और उसे भूल जाता जो दुनियां देख रही हैं पर वो नहीं कि वो मैले-कुचेले कपड़ों में, बिना जूतों के मोज़ों में, कुड़े के ढ़ैर के पास बैठा, शक़्ल पर बेवारसी और होंटों से निकलती बनावटी हँसी और शब्द।......
न जाने वो हर काम कल पर क्यों टाल रहा था और कल की सोच की वजह से ही शायद वहां पड़ा था। रोज़ एक नया कल पर आज की कोई छवि नही।
खैर मैं दुकानदार को बिना कुछ दिये और बिना कुछ लिये ही वहां से आगे बड़ गया। ये सोचता हुआ कि " सारे उलटे-सीधे दिल्ली में ही पड़े हैं। " उसे देखने के बाद और बाद में उसे सोचने पर मुझे मन ही मन हँसी आती रही कि
हालात चाहे कैसे भी हों पर उसका सपना छोटा नही था।
सैफू.
शख़्सीयत
Saturday, May 16, 2009
Labels: देखा-देखी , यादों की दुनियां...

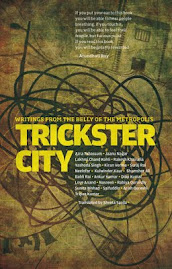
0 comments:
Post a Comment