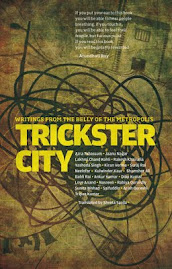एसा हमेशा से देखा गया है कि घूमने वाले के मन में एक लालसा होती है शहर को भीड़ में देखने की, वो भीड़ जो उसको भी अपने आप में समेट कर सामने वाले के लिए सिर्फ एक ही नाम छोड़ता है "भीड़"।
इसमे कई चहरे, कई मज़हब और कई तरह के माहौल जो कहीं-न-कहीं एक खाचे में अपने आपको छुपाए बैठे हैं जिसकी परख आप भी में उतरकर ही समझ पाते हो।
पुरानी दिल्ली- जो पहचानी जाती है भीड़ से, जिसे नवाज़ा जाता है यहां के माहौलों से, जिसे याद रखा जाता है यहां के चहरों और जगहों से, जिसे सुनाया जाता है यहां की आपसी बातों और समय से।
अपने आपको कई तरह के बदलावों में संजोती ये जगह कभी तो बदलावों को स्वीकार कर लेती है तो कभी बदलाव में जीने से किसी एसे डर को जोड़कर छोड़ देती है जिससे पुरानी दिल्ली हमेशा से लड़ती आई है- डर है खासियत के खो जाने का, डर है ज़हन से नाम मिट जाने का, डर है याद रखने की वजह बदल जाने का।
पर पुरानी दिल्ली की वाह-वाह आज भी यूहीं नहीं है! यहां के लोगों ने इसे हमेशा से रंगीनियत में रखा है समाज के साथ एक लम्बे समय से बहस में रहे हैं।
" ये बाज़ार है कोई आम सड़कें नहीं!”
यहां के माहौल और आवाज़े बाज़ार शब्द की बुनियाद पर ही रचे गए हैं।
शहर हमेशा से आपको आज़ादी से जीने का हक़ देता है लेकिन नियमबद्ध होकर और ये नियमबद्ध शब्द यहां कहीं-न-कहीं धूधला सा दिखता है, इसका मतलब ये नही कि इस जगह को शहर से कोई नाता नही, जुड़ाव तो हर छवि में दिखता है।
लेकिन कुछ पल में, कुछ कल में और कुछ आज में ये जगह कुछ अलग सी दिखती है।
सैफू.
वाह-वाह आज भी यूहीं नहीं है!
रंगीन होना क्या है?
दिवार पर बनी एक एसी तस्वीर जो न भगवान की है और न ही किसी मजदूर की वो न तो नेता है और न ही कोई भिखारी है पर वो तस्वीर किसी इंसान और मन की धारणा से मिल कर कोई काल्पनिक छवि को उभारती है। वो वोल-पेंटिंग दिवार की एक साइड को रंगीन बनाए हुऐ है पर गली की दिवार की रंगत से हमें क्या सीख मिलती है?
या उस पेंटींग से हमे क्या सीख मिल रही है मुझे समझ नही आता। रोज़ सुबह-शाम आते जाते उसे निहारता हूं,
सोचता हूं कि वो क्या बदलाव ला रही हैं निहारने और रुककर देखने वाले के लिए?
इतना सोचता हूं और अपने सवाल को अपनी ही बगल में दबा आगे बढ़ जाता हूं। क्योंकि हर बार सवाल के हैर-फैर मे मैं खुद हू उलझ जाता हूं और कुछ और ही सोचने लगता हूँ कि वो किसी की जिंदगी मे बदलाव लाए या न लाए पर वो पेंटींग दिवार की रंगत मे ज़रुर बदलाव लाए हुऐ है, रुककर देखने और दिवार पर सोचने का बदलाव लाए हुऐ है, जो हर दिवार के नसीब में कहां।
जैसे मेरे घर की दिवार जिसे मैने आज तक मन लगाकर नहीं निहारा पर जब भी कोई महमान घर पर आता है तो वो इसी चार दिवारी को निहारकर बोलते है घर तो बड़ा अच्छा है।
सैफू.
तुमसे पहले
नज़रे खाली थी तुमसे पहले, प्यास बाक़ी थी तुमसे पहले
तुम मिली तो लगा बहुत कुछ बाक़ी था तुमसे पहले।
काश मैं होता अकेला अगर तुमसे पहले
तो प्यार कर लिया होता मैंने भी तुमसे पहले।
शिकायत न होती अगर मुझे अपने ही बोले शब्दों से
तो आज इज़हार किऐ बैठा होता तुमसे पहले
नज़रों से बोलना, आँखों से सुनने का इशारा देना
आदत सी लगती है तुम्हारी
शौक होता अगर मुझे भी एसा
तो प्यार कर लिया होता तुमसे पहले।
नादान समझता था मैं अपने आपको इन मामलों में
अगर पहले ही भनक पड़ जाती मुझे जवानी की अपने आप में
तो काश कोई और होता मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले।
न जाने वो कैसी जरुरत बन गई थी मेरी
न बात करने पर बोखलाहट सी होती थी
ज्याद बात करने से बातों का सिलसिला खत्म सा लगता था
फिर भी मन में था- बात खत्म नहीं करुंगा उसके कॉल काटने से पहले।
मिलती थी जब भी तो फरमाईशों से झोली भर देती थी मेरी
मैं समझता रहा उसे, वो बोली एक दिन फोन पर
कुछ तो फाएदा हो मेरा, तुम्हारे रूठ जाने से पहले।
बे-फज़ूल की बातों से वक़्त गुज़ारते रहे हम साथ में
समझ नहीं आता- इन बातों का अन्त क्या है?
जिस दिन तुम्हें समझ आ जाए तो बताना ज़रूर
इस किस्से को खत्म करुंगा तुमसे पहले।
Labels: शिरकत
मेरी फिल्म के हीरो...
बचपन में अकसर हम कई तरह के गैम खेला करते थे। जैसे माचिस की डब्बियों से पत्ते बनाकर, सिगरेट की डब्बियों से पत्ते बनाकर एक-दूसरे की काट किया करते थे। जैसे गोल्ड फ्लेक पर गोल्ड फ्लेक का कार्ड रखने से बाज़ी के सारे पत्ते मेरे।
इन्ही कई तरह की गड्डियों में एक गड्डी और खेला करते थे हीरो-हिरोइनों के फोटो वाली गड्डी जो एक रूपये के A-4 पेपर से छोटे-छोटे फोटो कटिंग करके बनाया करते थे।
अकसर हम गड्डी खेलने डिलाइट सिनेमा की मुंडेर पर जाते थे हम सभी 12 से 15 तक की उम्र के दायरे में घिरे थे।
हम सभी दोस्त घेरा बनाकर गड्डी खेल रहे थे शाम का समय था, हमारा मस्ती करने का टाइम चल रहा था। वो भी उसी मुंडेर पर आकर बैठ गया- गन्दे-सन्दे कपड़े और हालत हमसे भी गई गुज़री।
हाथ में एक पुरानी सी कॉपी और कुछ कागज़ पकड़े हुए था तभी मेरी नज़र उसकी फटी-पुरानी कॉपी से निकलते हुए उस A-4 पेपर पर गई जो हमारे ही जैसा फोटो वाला था।
हमने उससे वो पेपर छिनने की नियत से पूछा- ये क्या है दिखाना?
वो आदमी- मेरी फिल्म के हीरो हैं।
मेरा दोस्त राजेश- दिखा कौन सा हीरो है?
उसने अपनी कॉपी को छाटते हुए बस कुछ कटिंग किये हुए फोटो दिखाए जिसमें से कुछ फोटो हमने पैरों के नीचे छुपा लिए थे। लेकिन उसने वो शीट हमारे हाथ में नही दी ना जाने क्या खास था उस फोटो पेपर में। कॉपी छाटते वक़्त हम सभी की नज़रे उसके हाथों मे मेली हो चुकी उसकी अपनी कहानियों पर थीं। कोई भी पन्ना एसा नही था जिस पर शब्द ना हों, अगर किसी पन्ने पर कहानी नही होती तो घुचुड़-मुचुड़ या काटी-पीटी होती शायद पूरी कॉपी भरी हुई थी और जो फोटो शीट को वो हाथ मे दबाए बैठा था नज़र जाते ही पता चला की उसने कुछ हीरो को चुन रखा था अपनी फिल्म के लिए ( सही का निशान लगा कर )
एक- दूसरे के बीच इस तरह के बरताव से हम छेड़छाड़ पर आ गऐ और अंड-शंड बोलने लगे...
राजेश- दिखा तो सही कौन है हीरों?
वो आदमी- मैं फिल्म की कहानी लिख रहा हूं।
राजेश- अच्छा... तो सुना क्या कहानी है?
वो हमसे छटपटाने लगा और हमारे बीच से जाने लगा तभी हममें से किसी की शरारत से वो कॉपी हमारे हाथ लगी।
फटी-पुरानी कॉपी के पहले पेज पर संजय दत्त का छोटा सा गड्डी वाला फोटो चिपका हुआ था और फल्म का नाम था रोटी, कपड़ा और मकान।
हमने उसकी कहानी को खूब मज़े ले-लेकर पड़ा उसकी कहानी उसकी ही अपनी रोज़मर्रा पर थी।
सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है।
सैफू.
Labels: यादों की दुनियां...
बहुत कुछ है इस फैलाव में.
अकसर देखा गया है कि ऐसी जगहें जहां शर्तो का माहौल एक दूसरे पर हावी रहता है वहां लड़कों का हुजुम बना रहता है जिसमें शातिर, चालाक या शर्त जितने का हुनर रखने वालों की भीड़ लगी रहती है। उस भीड़ को देखने वालों का कुछ और ही कहना होता है और खेलने वालों का कुछ और ही। इस कहा-कही में माहौल बत से बत्तर की छवि बना बैठता है समाज में, देखने, सुनने वालों में जिससे समाज दो अलग-अलग सोच से उस जगह को नवाज़ता है।
सुनने,बोलने वाले और देखने,खेलने वाले...
एसी बहुत सी छवियां जो पुरानी दिल्ली को उसी से जानने का नज़रिया देती हैं, पर उसमें उतर कर जीने वालों का कहना है कि "भाई सबके अपने अपने शौक होते हैं, जीने के तरीके होते हैं तो ये हमारा तरीका समझलो" और "ये तो खैल है हार-जीत चलती रहती है, उठना बैठना है जिससे टाइम पास हो जाता है।”
एसे बहुत से लोग हैं यहां जो इस जगह की अजीब सी रीत पर अपनी बात रखने से नही झिझकते, कोई यहां के माहौल से तंग है तो कुछ यहां के बरताव से, किसी को इस तरह के जीवन में जीना अच्छा लगता है तो किसी के पास कोई काम-वाम नहीं है तो उसे ये माहौल अच्छा लगता है मस्तिबाज़ी करने के लिए।
सब किसी न किसी तरह इसे अपनाए बैठे हैं कोई रात को तो कोई अपने काम से बचाया हुआ कुछ वक्त देकर।
गलियों और चौराहों पर टिकी नज़रें कभी तो दुआ-सलाम में झुकती नज़र आती हैं तो कभी वहां बना मजमा आपको भी शरीक होने का आमंत्रण देता नज़र आता है पर ये दुआ-सलाम और जुड़ने का आमंत्रण सिर्फ़ हमउम्र लड़कों तक ही सीमित है, क्योंकि यहां का बाहर लड़कों के लिए एक ऐसा स्पेस है जिसमें रहना, खड़ा होना, मीटिंग करना, खाना-पीना, बातें करना बिल्कुल ऐसा है जैसे वो जगह उनकी अपनी हो।
जगह से अपनापन बहुत है यहां के लोगों में जिसका आस-पास उनके स्वाद से जुड़ा हो, पसन्द से जुड़ा हो, या दोस्तों से जुड़ा हो।
Labels: संवाद
देखने में सब बाज़ार लगते है।
भीड़ में खड़े आगे बड़ने के इंतज़ार में लम्हें बे-इंतज़ार लगते हैं।
कोई इधर झाके, कोई उधर झाके
देखने में सब बाज़ार लगते हैं।
चीज़े तितर-बितर है, लोग चलने में मशरूफ लगते हैं
कदम ना बड़े आगे तो वो बातों में लगते हैं।
निकल पड़े हैं सब घरों से, सजने को बेकरार लगते हैं।
देखने में सब बाज़ार लगते हैं।
गलियां बन गई हैं छटने के रास्ते
सीधी सड़क पर सब चलते से लगते हैं।
आवाज़े बन गई हैं रुकने के बहाने, आपस में सब बतियाते से लगते हैं
देखने में सब बाज़ार से लगते हैं।
रह गया हैं कोई मंज़र पुराना
ठिकानों की सब तलाश में लगते हैं
बेफिकरी में घुसते जा रहे हैं सब, एसे में सब बेकार लगते हैं
देखने में सब बाज़ार लगते हैं।
कहीं खान-पान का मेला तो खरीदारी का ज़ोर
सब एक-दूसरे की ज़रूरत सी लगते हैं।
ना हो ज़ोर किसी पर, तो वो घूमने में लगते हैं
देखने में सब बाज़ार लगते हैं।
न जाने, अंजाने रिश्तों को लोग अपना बनाने
क्यूँ निकल पड़ते हैं
सब एक-दूसरे में भूले-बिसरे से लगते हैं
देखने में सब बाज़ार लगते हैं।
पकड़कर हाथ किसी का रिश्ते की नई शुरूआत में दिखते हैं
मान जाता है कोई तो बातों की पहल में लगते हैं
देखने में सब बाज़ार लगते हैं।
कैसे कहूं मैं भीड़ इसको
ऊपर से देखने का धोका भी हो सकता है
उतर कर बाज़ार में क्या कह सकता हूँ मैं
देखने में सब बाज़ार लगते हैं?
Labels: देखा-देखी
कोई रिवाज़ नहीं था, बस यूहीं...
हमेशा से जगह अपने अंदर कई बातें, कई किस्से छुपाए बैठी होती है। अलग ज़ुबान और अलग अलग किस्से-कहानियाँ बदलती पीढ़ी में भी बातों और यादों के ज़रिये अपना सफर बरकरार रखती हैं। लोगों का दोहराना और बातों-बातों में बातों का फिसल जाना चलता रहता है जिससे कई महफिलें और मजमे अपने आपको रोज़ना की दौड़ में जमा पाते हैं। एसे ही बातों-बातों में पुरानी दिल्ली के भी कई किस्से तरह-तरह की ज़ुबानों और उम्र के साथ सामने आए कुछ सुनने में इतने रोमांचक लगते कि मानों बस सुनते ही जाओ तो कुछ उम्र दराज़ आवाज़ में दम-खम के साथ पेश आते हैं।
जामा मस्जिद चौक का ख़म्बा...
हम उसे पुराने दोर का खम्बा भी बोल सकते है।
कई साल पहले जामा मस्जिद चौक पर एक बड़ा सा ख़म्बा हुआ करता था जो इस समय हमारे साथ नही रहा। सुनने में आया है कि उसे सड़क बनाते वक़्त हटा दिया गया था क्योंकि वो सड़क को चौड़ा करने के काम मे आड़े आ रहा था। हमारा मानना था कि उस ख़म्बे के बारे में कोई बुजुर्ग ही हमें अच्छा किस्सा सुना सकते हैं क्योंकि समय के साथ जी चुके लोग समय को उसी रंग में दिखाते हैं जो उसका रंग था। लेकिन जब कई रंग की कहानियों से किसी पन्ने को रचा जाता है तो उसे हम रंगीन कहते है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और उसी रंगीन पन्ने की तलाश में हम पहुचे चितली क़बर चौक जहां रोज़ रात कुछ बुजुर्ग बाज़ार की दुकान बन्द होने के बाद उसके तख़्त पर अपनी पुरानी यारी-दोस्ती के किस्सों से, कुछ आज से कुछ कल से वहां महफिल सजाते है। मिलने की सोच थी कि अगर हम उनसे ख़म्बे के साथ जुड़े लम्हों के बारे में पूछें तो कई तरह की कहानियाँ- यादें और घटनाए सामने आएंगी।
ये सब बुजुर्ग आस-पास से इकठ्ठा होकर इस जगह में मिलते है सब एक-दो साल कि छोट-बड़ाई से एक-दूसरे के साथ रहते आए है जिनमें से कुछ जान-पहचान के हैं तो कुछ अंजान लोग, आते-जाते इनसे दुआ-सलाम का सिलसिला तो सालों से चला आ रहा है पर कुछ नए सिलसिलों की शुरूआत इस बार हुई है।
लगभग सभी सफेद कुर्ते-पेजामें की पोशाक में है जिसमें टोपी भी शामिल है। इनका आपसी तालमेल बहुत ही शांत तरीके से माहौल में दिखाई देता है जिसमे से शौर और हा-हा-ही-ही कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता, पास जाने पर सबके चहरों पर खिलखिलाहट जरूर दिखती है। इनके बीच शामिल होने के लिए न जाने क्यों किसी तैयारी की कमी महसूस हो रही थी पास जाने पर समझ आ गया था कि तैयारी बस अपने रवइयें की करनी थी। क्योंकि जब कोई न-पसंद हो जाता है तो उसका उनके बीच में रहना न-मुमकिन हो जाता है।
हम – अस्सलामु अलेयकुम.....
( सलाम ही महफिल में आपको इज़्ज़त देता है, आपके सलाम के जवाब के साथ )
वालेयकुम अस्सलाम- सबकी आवाज़ में जवाब हल्की सी गूज़ बनकर सुनाई दिया।
दुआ-सलाम के बाद हमने उनसे कुछ पूछने की इजाज़त मांगी तो जवाब "पूछो-पूछो" में मिला।
मैं – आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, ( किसी एक चहरे की तहफ देखते हुए )
अब्बा जामा मस्जिद चौक पर पहले एक ख़म्बा हुआ करता था उसके बारे में जानना था कि वो कब से कब तक था और लोग उसके साथ कैसे जिया करते थे?
"हम उनकी सुनाई हर एक बात को बड़े ही एहतियात से सुन रहे थे"
अब्बा - हां था। और वो अब का थोड़ी न था, हम खुद उसे अपने बचपन से देखते आए थे।
मैं - कैसा दिखता था वो ख़म्बा ?
अब्बा - अरे वो बहुत काला था चौड़ा और लम्बा भी था उसके निचे गोल चबूतरा बना हुआ था जिस पर हम भी जाकर बैठ लिया करते थे।
अब्बा काफी बुजुर्ग थे इसलिए उन्हें अब्बा कहना अच्छा लग रहा था और उनकी बातों से लग भी रहा था कि वो बहुत कुछ बता सकते है, अब्बा की आवाज़ में ज़रा सी भी झिझक नहीं थी किसी भी बात को बताने में।
मैं - हां हम उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि लोग उस खम्बे को अपनी ज़िंदगी में कैसे जिया करते थे?
अब्बा सबकी तरफ देखते हुए बोले- सबकी तो नहीं पता पर हां उसका अपना बस एक ही किस्सा है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है जितने भी हम बैठे हैं तुम्हें छोड़कर।
यहां के किसी भी बुजुर्ग से पूछ लेना कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो बारात कहां से घूमाकर लाए थे... किसी पुराने आदमी से ही पूछना जो जामा मस्जिद इलाके का हो हमारी तरह।
"अब्बा का खुद के साथ, साथ बैठे सभी को पुराना कहने पर सब हसने लगे... एक-दूसरे की तरफ हँसी की दावत देते चहरे हमें भी हँसी के कुछ पल दे गए अपने बीच।"
मैं - बारात घुमा कर लाने का क्या रिवाज़ था ?
अब्बा - कोई रिवाज़ नहीं था, बस यूहीं...
मैं - यूहीं मतलब ?
अब्बा - हम कितनों की ही शादियों में नाचे, कुछ अपने, कुछ अंजान पर सबकी एक दिशा हुआ करती थी बाज़ार से होकर जामा मस्जिद के ख़म्बे तक फिर ख़म्बा घूमकर बाज़ार से होते हुए वापस घर। सबके साथ इतना सोचा नहीं था कि ये क्या रिवाज़ है? पर जब खुद की शादी पर बराती खम्बे की ओर चलने लगे तो चलने से पहले मैंने अपनी अम्मी से पूछा- अम्मी ख़म्बे तक क्यू जा रहें है हम? हमे तो बस पास मैं ही जाना है, कोई रिवाज़ है क्या ? तो अम्मी ने कहा- अरे बस यूहीं।
जब से मैं भी इतना ही जानता हूँ कि वहां शादियों पर लोग चक्कर बस यूहीं लगाया करते थे।
बराबर में बैठे बुजुर्ग ने भी इसमें अपनी बात जोड़नी चाही।
अंकल - चक्कर लगाना कोई जरूरी नहीं था मर्ज़ी वाली बात थी पर अगर कोई खम्बे का चक्कर नहीं लगाकर आता था तो बरातियों में से कोई न कोई पूछ ही लिया करता था- ख़म्बे का चक्कर क्यू नहीं लगाया?
कुछ बेफज़ूल की बात बता कर इस सवाल को टाल दिया करते थे तो कुछ सोचते थे लगाने में कोई हर्ज नहीं था लेकिन बात कुछ और थी। हमें तो लगता था कि जैसे ये कोई बादशाही वक़्त की रीत की तरह चल रहा था।
मैं - वैसे वो खम्बा वहां कब से था ?
अब्बा और कइ ज़ुबानों ने आगे-पीछे बोलते हुए जवाब दिया- हम सभी अपने बचपन से उसे देखते आए है और शायद वो पुराने वक़्त से ही है।
अब्बा - पहले उसके पास से होकर ट्रैन गुज़रा करती थी, चावड़ी, सदर, नई सड़क, यहां और लाल किले जैसी कई जगह से होकर वो पुरानी दिल्ली में घुमा करती थी वो जामा मस्जिद के इस ख़म्बे पर भी आकर रुकती थी पर वो अपना एक वक़्त हुआ करता था मोज-मस्ती का, घूमने-फिरने का।
अच्छा तो अब हम इजाज़त चाहते है अभी के लिए पर हम आते रहेंगे और हां अब्बा ये ट्रैन वाली बात continue रखेंगे।
ये कहते ही सब हसने लगे और माहौल में हा-हा-ही-ही की आवाज़ आज पहली बार सुनाई दी।
सैफू.
Labels: महफिलों के बीच से... , संवाद
रमज़ान-ऐ-मुबारक
साल का एक अकेला एसा महीना जो चमका देता है पुरानी दिल्ली को "रमज़ान-ऐ-मुबारक" रमज़ान की रोनक को अगर महसूस करना हो तो या उसे खुद में शामिल करके मज़े लेना हो तो पुरानी दिल्ली से बढ़ियां जगह और कोई हो ही नही सकती। चकाचौन और भीड़-भाड़ वाला माहौल पुरानी दिल्ली को देखने लायक बना देता है "कहते हैना- हीरे में भी खूबसूरती तभि आती है जब उसे निखारा जाता है, उसे किसी रूप में जड़ा जाता है।
लोगों का मिलना-जुलना, 24 घन्टों की चहल-पहल और बाज़ार- देखने और घूमने का मज़ा बनाए रखते हैं।
घूमने का मज़ा यहां हर कोई उठाता है घर से अगर अफतार का सामान लेने भी निकलना होता है तो वो मज़ा बरकरार रहता है। इधर-उधर ताकना चलता रहता है यहां माहौल दोनो पार्टी के लिए एक जैसा है, लड़कियां भी बहुत मज़े लेती हैं बाज़ार के- ये पता होते हुए भी कि बाज़ार में छेड़छाड़ लाज़मी सी बात है सज-धज के निकालती हैं।
ताका-ताक़ी बराबरी की होती है कुछ बे-खबर होते हैं तो कुछ ज्ञानी इन मामलों में पर इस बीच बाज़ार धड़ाके से खरीदारी में जुटा होता है।
हर किसी को जल्दी है ईद की तैयारी की तरह-तरह के सूट, पेंट, शर्ट-टी-शर्ट, बेल्ट, बुंदे, चूड़ियाँ... ये-वो अगड़म-सगड़म तरह-तरह की तैयारियों से भरा बाज़ार, अपनी और खरीदारों की ज़रुरतों से बना बाज़ार, इधर-उधर की तरह-तरह की बातों में लगा बाज़ार कभी त्योहारों तो कभी सण्डे को सजता बाज़ार कभी उसने बोला चलो बाज़ार कभी मैंने बोला चलें बाज़ार...
खैर ये तो माहौल की बात है रोनक इसकी खासियत है और भीड़-भाड़ एक आम बात लेकिन लोगों का सड़कों पर रातों का गुज़ारना बाज़ार को और होसला देता है देर रात तक सजने का। बरसों से चला आ रहा है ये रिवाज़ कि यहां रोनक को, आवाज़ों को, चहल-पहल को, मिलने-जुलने को ही ये जगह अपनी खासियत मानती है।
और आज भी यहां के लोग उसी अंदाज़ में रमज़ान की रातों को गुज़ारतें है जैसा उन्होने देखा उसी को अपनाया। ज्यादातर लड़के रातों को मस्ती करते है, कोई घूम-घूमकर तो कोई मंडली बना कर जिसमे यार दोस्तों की हसी मज़ाक से आस-पास मे जान रहती है।
जामा मस्जिद सजता है उनके लिए जो आते हैं वहां ये सोचकर चलो चलते हैं जामा मस्जिद घूमने अभी वक़्त है सेहरी में, अज़ान की गूंज बहुत खास है यहां के लिए- अज़ान होते ही कुछ घरों से कुछ सड़कों से लड़के आदमी सिमट जाते हैं मस्जिदों में, सड़कों पर बचतें हैं बस बे-नमाज़ी या औरतें जो उनके लिए शोपिंग का सबसे अच्छा टाइम है। पर ये सकून सिर्फ कुछ लम्हों तक ही रहता है उसके बाद फिर एक भीड़ बाहर आती है और माहौल की वो आवाज़ें, चहल-पहल, आवारग़ी जिसे हम रोनक कहते है वो रचा जाता है।
सैफू.
Labels: देखा-देखी
बदलेगा जामा मस्जिद इलाके का चेहरा.

पिछले कई सालों से M.C.D सरकार के आगे ये गुहार लगा रहा था कि उनको जामा मस्जिद क्षेत्र को सुधारने की अनुमति मिले और इस साल इस गुज़ारिश को स्विकार लिया गया है।
कई नियमों के तहत और बदलावों को सोचते हुए कई कढ़े कदम उठाये जाएंगे और M.C.D की अपील में ये बात साफ हो गई है कि यहां के कारोबारियों और छोटे-मोटे कामकाजो से अपनी रोज़मर्रा चला रहे लोगों का भी ध्यान रखा जाएग। लेकिन इन सब के पीछे का सच यही है कि छोटे कारोबारी लोग विकास के दौरान रोंध दिए जाएंगे।
बदलाव जामा मस्जिद इलाके की रोज़मर्रा में ही नहीं वहां की रोज़मर्रा से जुड़े लोगों की रोज़मर्रा में भी आएगा।
ये ज़ाहिर सी बात है- मीना बाज़ार, जामा मस्जिद गेट नम्बर 1 और 2 के आगे जितने भी छोटे-मोटे कामों से जगह सजी रहती है उनको सुधार के दौरान जगह को चौड़ा और सुंदर दिखाने के लिए हटा दिया जाएगा।
स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन ने इस योजना को 'महात्वाकांक्षी योजना' बताया है और कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है कि जामा मस्जिद, लाल किला, चाँदनी चौक को उनका वास्तविक रूप दिया जाए और जहां तक हो सके आस-पास के कारोबारीयों का भी ध्यान रखा जाए।
चेयरमैन ने इस बयान में ये बात साफ कर दी है कि ये निर्णय हाई कोर्ट का है। इन योजना से पहले हाई कोर्ट ने M.C.D से कई मानदंडों और रिपोर्टों की मांग की है और इस मांग के पीछे हाई कोर्ट ये चाहता है कि रिपोर्ट को देखकर वो ये बात साफ करले कि इस पुनर्विकास के निर्माण कार्यों से इस एतिहासिक स्थलों पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। और जहां तक कोशिश की बात है- M.C.D इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि जामा मस्जिद के मुख्य ढ़ाचे को सुरक्षित रखा जाऐ।
सैफू.
Labels: संवाद
खासियत ही पहचान है।
खान-पान मे पुरानी दिल्ली किसी से पीछे नहीं है। शाकाहारी, मासाहारी, नाश्ता, चखना, सेहरी कई प्रकार के खान-पान से सजी पुरानी दिल्ली अपने आपको और भी लुभावक बनाए रखता है।
आते-जाते लोगो को ये जगह इतनी लुभावक लगती है कि बिना चखे आगे बढ़ने का मन नहीं करता और कोई जब चखने बैठ जाता है तो बिना पेट भरे उठा नहीं जाता।
यहां की लज़ीज़ बिरयानी और तरह-तरह के नामों से मशहूर नहारी अपनी खास पहचान बनाए हुए है पर यहां मासाहारी लोगों को ज्यादा भाता है क्योंकि जैसे लोग वैसा पकवान कहीं तीखा तो कहीं मीठा, पनवाड़ी के ठिए-दुकानों से लेकर रेड़ियों तक का माहौल रुकने-ठहरने का आमंत्रण एसे बाटते हैं जैसे कोई चुम्बक-चुम्बक को खैचता है।
इन सब चीज़ो, माहौल में आकर्षण अपना खैल रच रहा है जिसकी समझ बहुत गाढ़ी है। नऐ चेहरों को ये बहुत देर से समझ आता है पर धीरे-धीरे बितते समय में चीज़े छटती जाती है कुछ मन भावक तो कुछ पराई होकर रेह जाती है लेकिन चीज़े, स्वाद और चलते बाज़ार अपनी पकड़ को बनाए रखते हैं और इनको वो पकड़ देता है यहां का माहौल जो चाहता है कि एसी चीज़े टाइम-बे-दाइम बरकरार रहें जिससे पुरानी दिल्ली की पहचान में कोई बदलाव न आए क्योंकि जगह की पहचान ही जगह का वजूद बनाती है।
वक्त-बे-वक्त बनते गुच्छों की रचनाऐं इस जगह को रचनात्मक बनाए रखती है। सीधी रस्सी की तरह दिखती यहां की रोज़मर्रा में कई एसे बल हैं जिसे दूर से देखकर परख पाना मुश्किल है इन बलों की परख उन्हीं को है जो इस जगह को रचते हैं।
सैफू.
मेरा प्यार...
फिर क्यों रात को फोन पर वो मुझे आई लव यू कहती है।
आवारा हूं मैं, बोलकर कभी तो वो मुझे जगहों में कोसती है,
न जाने फिर क्यों रात को फोन पर वो मुझे आई लव यू कहती है।
जब गलियों मे रोककर बोलता हूँ उसे जान, जानू, सुनो तो,
तब कोई जवाब नहीं देती,
पर क्यों रात को फोन पर "जान बोलोना न मुझे" वो कहती है।
तुम कितनी कोमल हो, अच्छी हो, खूबसूरत हो रोज़ कहने से झिझकता नहीं मैं,
लेकिन हर बार फोन करने के बाद ही क्यों ये बातें याद आती हैं।
कई चहरों से प्यार करता हूं मैं, रोज़ एक नया चहरा ढूढ़ता हूँ,
उसका चहरा तब सामने आ जाता है जब फोन पर मिस-कोल देती है।
कितना प्यार करते हो मुझसे?, ऐसे सवालों में मुझे घेरे रखती है,
क्यों वो मुझे फोन पर बचकानेपन में आई लव यू कहने पर मजबूर कर देती है।
कितनी बार सोचता हूँ कुछ खिला-पिला दूंगा तो प्यार बढ़ जऐगा,
कहीं घुमा-फिरा दूंगा तो प्यार बढ़ जाऐगा,
पर जब भी मैं गली से गुज़रते उसके कदमों मे अपने कदम मिलाता हूँ,
तो वो "कोई देख लेगा" ये कहकर गली ही बदल लेती है।
कभी खिड़की से कभी छत पर वो रोज़ मिलने आती है, इशारा फोन का बनाती है,
रात को फोन पर कहता हूँ "कहीं घूमने चलो" तो बहाना परेशानी बताती है।
दो दिन बात न करो तो फोन पर बड़ा चिल्लती है, कहती है
"पता है कितनी परेशान हो गई थी मैं"
मैं बातों-बातों में कहता हूँ रिचार्ज करवा दूं क्या तुम्हारे फोन का,
तो जवाब हाँ मे बताती है।
कभी दुपट्टे में तो कभी बुरखे मे जब वो बाज़ार मे निकलती है,
उसकी नक़ाबी आँखों मे, मैं उसे पहचान लेता हूँ,
मैं उसके इतने करीब कैसे ये देखकर वो सर्रा सी जाती हैं।
मैं रात को फोन पर पूछता हूँ "अपने बारे में भी कुछ बताओ"
तो वो घर के बाद मुझसे प्यार करती है, बड़ा ही शर्माकर बताती है।
एक घंटा, दो घंटे, कई घंटे बातचीत का सिलसिला चलता रहता,
फोन थका, मैं थका क्या तुम थक गई हो, "सोना कब है?"
तो वो टाईम सुबह होने तक बताती है।
कई बार उसका हाथ पकड़ा तो वो छुड़ाकर भाग जाती है,
सीढ़ीयों पर उसे जकड़ा तो वो सिमट सी जाती है,
जब रात को उससे फोन पर पूछता हूँ "कैसा महसूस हुआ था तुम्हें?"
तो वो उसी को प्यार बताती है।
उस प्यार का क्या फाएदा जिसमे मिलन न हो, एक दूसरे से मिलने वाली सर्रसराहट न हो,
मेरी इस बात पर न जाने क्यों बैशर्म हूँ मैं जताती है।
डरती है मिलने से, करीब आने से, कहती है तुम डाकू हो गांव लुट जाऐगा,
फिर सज-सवर कर क्यों निकलती हो जब गांव की फिक्र है,
तो वो दूर रहने मे ही भलाई बताती है।
पल-भर में चहरे के बदलते भावों से वो ये एहसास कराती है
"मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ"
फिर क्यों रात को फोन पर वो इन बातों को सिर्फ दिखावा बताती है।
मैं सोचता हूं कि ये मेरी सेटिंग है, वो कहती है तुम मेरे जानू हो,
मैं पूछता हूँ शादी करोगी मुझसे ?
तो क्यों वो फोन का "ऑफ बटन" दबाती है।
Labels: देखा-देखी , महफिलों के बीच से...
क्या नाम है तुम्हारा ?
वो घबराई, हिली-डुली बोली - "चल आवारा"।
घर के नीचे खड़ा रहता था शाम होते ही उसके,
वो आती थी वहां जहां था उसका चौबारा।
एक दिन फिर उसे सीढ़ियों से उतरते देखा, पूछा- "क्या नाम है तुम्हारा?"
वो बिना कुछ बोले सीढ़ीयों पर चढ़ गई दोबारा।
जिस दिन ना दिखे वो गली में, मैं रास्ता तकता रहता था,
अपने में बड़बड़ाता रहता था, बस एक बार दर्शन हो जाए दोबारा।
नज़रों में उसकी जैसे जादू सा था, मन करता था देखूं उसकी आखों में
एक रंग बदलता आसमां नज़र आता था मुझे उसकी झपकती आँखों में।
वो शाम को आती थी, मेरे आगे से सीधी निकल जाती थी,
शायद उसके भी मन मे आया होगा " पूंछू क्या नाम है तुम्हारा?"
बोरियत जैसा कोई शब्द नहीं था मेरी जेब में, जेबों में हाथ डाले खड़ा रहता था,
वो आएगी ये इंतज़ार था, तब मैं पूछूंगा "क्या नाम है तुन्हारा?"
वो मिली मुझे पल्ली गली में, बोली- "रोज़ मेरे घर के नीचे क्या काम है तुम्हारा?"
मैंने उसका हाथ पकड़ा, बोला- "आई लव यू ,अब क्या जवाब है तुम्हारा?"
कहने लगी- एक दिन गली के कोने में लेजाकर, मैं कोई प्यार-व्यार नहीं करती,
मैं तंग हूँ तुमसे, पीछा क्यों करते हो मेरा,
मैं मुस्कुराया, बोला- एक बार बात करनी थी तुमसे बस काम हो गया हमारा।
वो नज़रे झुकाकर जाने लगी जब, मैंने धीमे से पूछा "क्या नम्बर है तुम्हारा?"
वो मुस्कुरा कर बोली- रहने दो, कुछ नही रखा इन चीज़ों में,
मैं भी मुस्कुरा कर बड़बड़ाया- यही तो काम है हमारा।
मुझे यकीन था वो मिलेगी मुझसे ज़रूर क्योंकि अब प्यार एक-तरफा नही,
हो चुका था हमारा।
कल के दिन इंतज़ार की वजह बदल जाएगी
वो आएगी अब मेरी गली में पूछेगी "क्या नाम है तुम्हारा?"
रात मे ना जाने कहां...
गली के बाहर लगे चार लड़कों के मजमे ने अपनी आपसी बातों से आस-पास को अपनी गूंज से महका रखा है, कोई उनको मस्त तो कोई उन्हें छिछोरा बड़बड़ाता हुआ निकल जाता। पर वो चारों अपनी ही मस्ती से माहौल मे वो गर्माई बनाऐ रखते जिससे बातों को सुनाने और सुनने का मज़ा बना रहता।
यहां हर गली, हर नुक्कड़ ऐसी महफिलों का भंडार लिए हुऐ है और हर एक महफिल अलग माहौल और बातें।
कहीं किसी दुकान के बाहर तो कहीं किसी बंद दुकान के चबूतरे पर तो कहीं इन चारों की तरह कही किसी गली के नुक्कड़ पर। ये सब यहीं आस-पास के यार-दोस्त हैं जो आस-पास की किसी भी बैठक पर बैठकर बातें बतियाते हैं।
जैसे किसी तख्त, खाली खड़ा रिक्शा, रेड़ी या चबूतरा। ये रोज़ नई बातें और रोज़ एक नई महफिल को अलग ढ़ंग से सजाते हैं।
कभी 4 तो कभी 6 तो कभी पूरी टोली पर आज ये चारों मस्ती भरे अंदाज़ मे एक दूसरे से मिले हैं।
ना मैं इनका नाम जानता हूं और ना ये जानता हू कि ये रहते कहां हैं ? पर इनकी आपसी बातों की गूंज ने मुझे इनकी ओर खैंच लिया
(सोचता हूं काश मेरे भी कई दोस्त होते और मैं भी इनकी तरह बने एसे मजमों में शरीक हो पाता)
ये चारों एक दूसरे से हंस-हंसकर बातें करते, कभी एक के हाथ बड़ाने पर दूसरा उसके हाथ बड़ाने को समझ उसे ताली देता तो कभी आपस मे ही एक-दूसरे तो उंगली दिखा कर हंसते।
ये इनकी आपसी समझ है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़े रखती है, इनका रोज़ कोई नई जगह को तलाशना और मिलना कई संदर्भो मे बहा ले जाता है। एक दूसरे को जान पाना और मिज़ाज़ को समझना रोज़ नई कहानी को इनकी रोज़मर्रा से खींच लेता है।
सुबह से शाम तक की रुटीन को अपनी रात की मण्डली मे उतारना रोज़ का काम बन जाता हैं। ये चारों भी जब एक दूसरे की तरफ इशारा करके हंसते है तो मुझे इनका साथ बिताया हुआ पल दिखाई देता है। जब ये हवा मे बातें करके हंसते है तो मुझे इनसे जुड़ी कई ज़िन्दगियाँ नज़र आती हैं और जब ये हंसते-हंसते चुप्पी का माहौल साध लेते है तो मुझे इनके बीच का संवाद नज़र आता है कि ये महफिलें चीज़ो, माहौलों, शख्सों को सिर्फ़ हल्के मे ही नही गहराइ से भी लेना जानते है, जो इनकी जिंदगी में आते हैं, मिलते हैं और कुछ पल बाद सिमट कर खो जाते हैं।
मैं रोज़ अपनी गली के बाहर इन्हे कहीं खड़ा तो कही बैठा देखता हूं और ये रोज़ इसी जगह को चुनते है शायद कुछ समय के लिए उसके बाद या उससे पहले ये इस रात मे ना जाने कहां नज़रों मे आते होंगे।
सैफू.
Labels: महफिलों के बीच से...
चाय, बातचीत और रोज़
कई चलती कहानियों, बातों और किस्सो को अपने मे समेटे ये चाय की दुकाने हमसे भी हमारे रोज़ के कुछ मिनट मांग बैठती ह। इसका लुभावक तरीका और खुला मिज़ाज़ अपनी ओर खैंच लेता है। इसकी खुद की कहानी में कई जोड़ हैं जो आता है वो अपना कुछ टाईम इसमे जोड़कर इसकी डोर को और लम्बा कर देता है।
कई सालों से लोगों के बीच उसी पुराने अंदाज़ में आज भी ये दुकान उसी तरह पेश आती है जैसे बीते कल मे साथ थी। यहां आते लोग कभी-कभी कह बैठते है कि "हम यहां तब से आते है जब यहां 1 रू॰ की चाय मिला करती थी, आज 5 रू॰ की चाय है पर अब भी वैसे ही चाय पीते हैं जैसे 1 रू॰ में पिया करते थे।"
"सच बताऊ तो चाय-वाय तो बस एक बहाना है बस यहां बैठने का जो मज़ा है जो हमारी सालों की बैठक है, वो मज़ा और कहीं नही"
इनका नाम मौ॰ अय्यूब है कम से कम 45 साल के लगते हैं, इनकी बातचीत में बहुत मिठास है और इनकी मिठास की तारीफ तो दुकान के मालिक फिरोज़ भाई भी करते हैं। इनकी और अय्यूब भाई की खूब पटती है, ये सालों से इसी मिठास को अपनी आपसी बातचीत मे बरकरार रख पाऐ हैं।
अय्यूब भाई आज भी आऐ हुऐ थे हमारे आने से पहले ही वो कुर्सी पर अपने कुर्ते को उडेसे बैठे थे। हम तीन लोग सलीम, इशान और मैं रोज़ रात 10 बजे के बाद चितली क़बर चौक पर चाय पीने जाते हैं।
चितली क़बर चौक से अंदर होकर हवैली आज़म खां में ये चाय की दुकान है। अय्यूब भाई हमेशा केश-काउंटर के बराबर वाली कुर्सी पर ही बैठते है जिससे कि बातचीत का सिलसिला लगातार बना रहे।
आज भी वो वहीं बैठे थे, हम तीनों भी उस चार लोगों को समेट लेने वाली टेबल मे सिमट गऐ, अय्यूब भाई हमारे साथ और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठै थे।
अय्यूब भाई : यार आज घर में बड़ी किच-पिच हो रही थी, छोटी बहू फज़ूली बात पर हंगामा मचाऐ हुऐ है, अरे ये भी कोई बात होती है?
दुकान का मालिक जिनका नाम सिराज है।
सिराज भाई : अच्छा?
उनके अच्छा बोलते ही अय्यूब भाई, सिराज भाई के कान मे कुसुर-फुसुर करने लगे।
इशान सलीम से बोला कि यार ये बताओ कि आज चाय कौन पिला रहा है?
मेरा सारा ध्यान अय्यूब भाई पर था कि यही तो थे वो जो उस दिन कह रहे थे कि मैं यहां तब से आता हूं जब यहां 1 रू॰ की चाय मिला करती थी। उनको देखकर लगा कि अय्यूब भाई का यहां से चाय का कोई रिश्ता नहीं है और ना ही जगह का कोई आकर्षण इन्हे यहां खैंचता है, इनका और भाई फिरोज़ का आपसी रिश्ता ही एक-दूसरे को बांधे हुऐ हैं और सुनने-सुनाने का ये रिश्ता सालों से महफूज़ है लेकिन सिर्फ इस जगह में।
तभी सलीम बोला भाई तू पिला रहा हे चाय?
मैं : हां बनवा लो दो बटा तीन पर मेरे पास सिर्फ़ 7 रू॰ हैं, 3 रू॰ कोई ओर देना।
दुकान ज्यादा बड़ी नही है, चार टेबल और एक टेबल पर चार लोग, मतलब 16 शख्स एक साथ इस महफिल मे शरीक हो सकते हैं। कोई नया डिज़ाइन नहीं है यहां वही पुरानी टेबल-कुर्सियां से सजा माहौल, वही सालों पुराना काउंटर और वही पुरानी दाना-दाना करके बनाई हुई पब्लिक।
तीन कर्मचारी...
पहला : 17-18 साल का लड़का, चाय का काउंटर संभालता है
दूसरा : 12-13 साल का बचपन, पानी के गिलास आते ही आगे रखना और चाय के झूटे गिलास रखने-उठाने का काम करता है।
तीसरा : 40 से 45 साल के उम्रदराज़ ओदे के साथ, वो हर आने वाले का स्वागत उनसे से पूछकर करते है कि
"कितनी चाय ?" वो ओर्डर लेने क काम करते है, इन्ही तीनो का एक काम और होता है बाहर की पब्लिक को संभालना जिसमे दुकान, ठिऐ, और कहीं किसी नुक्कड़ पर लगे मजमे शामिल होते हैं।
सभी कुछ एक आम चाय की दुकान की तरह है जहां लोगो का रुकना-बाहर निकलना चलता रहता है। पर फिर कही ओर जाने का मन नहीं करता। रोज़ इन्ही टेबलों पर टिकाने का मन बनाऐ हम घर से निकल पड़ते हैं।
यही सोच कर कि अपने अड्डे पर चलकर चाय पियेंगे।
सैफू.
Labels: महफिलों के बीच से...
रास्ता अभी बाकी है।
चहरा लटकाए मैं अपने आपको कोस रहा था। इधर-उधर देखा कोई नहीं दिखा तो अपने आपको ही देख लिया। काश कोई दिख जाता तो सकून तो होता कि इस तन्हा रात में मैं अकेला नहीं हूँ।
पर मैं अकेला ही था, न अपने आपसे बातें करने का मन था और ना ही किसी ओर से पर फिर भी किसी को देखने की आस थी जो मुझे इस अकेलेपन से बाहर खींच सके।
लेकिन मैं अपने आपको क्यू कोस रहा था ? सिर्फ़ इस वजह से कि मेरा रास्ता अभी और भी है, और मैं चल रहा हूँ। न भागता हूँ और न छलांग लगाता हूँ, कहीं टकराता हूँ तो गिर जाता हूँ एक बार नहीं कई बार और जिस चीज़ से मैं बार-बार टकराता हूँ तो उसे लांगता क्यू नहीं?
सवाल तो कई लाई है ये रात पर जवाब नही लाई, अपने कालेपन के साथ-साथ मेरे जवाबों पर भी काली परते चढ़ा रखी हैं इस रात ने।
बार-बार आस-पास का संनाटा मेरे कानों में आकर सिमट जाता और मैं फिर एक बार घबरा जाता ये सोचकर कि
" काश कोई और भी होता इस रात में। "
सैफू.
Labels: संवाद
"लोगो की शिरकत"
पुरानी दिल्ली के कई कौने अपनी-अपनी खासियत से मशहूर हैं। और उनका मशहूर होना यूही नहीं बना वो बनना चला आ रहा है पीढ़ीयों से, लोगों की पसंद से वो पसंद जो जगह और लोगों के बीच के धागे मे गीठा लगाऐ हुऐ है।
जिसे खोलना या खींच कर तोड़ देना आसान नहीं है। सरकार ने ऐसी कई उम्मीदे लगाई हुई थी पुरानी दिल्ली को लेकर पर बड़े-बूड़ों का साथ और लोगों का जगह से एक खास रिश्ता हमेशा सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरता आया है।
जामा मस्जिद की मरम्मत से लेकर बाज़ारों की रोनकों तक सरकार ने हाथ फैरना चाहा जिसे कुछ चीज़े धुंधली हो जाऐ लेकिन लोगो का जगह से रोज़ का जुड़ना और माहौल के बनने से बनाने की परिक्रिया मे रेहना सरकसर को पुरानी दिल्ली को छूने तक नहीं देता ।
सरकार चाहती है कि बदलती दिल्ली में पुरानी दिल्ली का भी वजूद बदले, चल रही पीढ़ी को नए नियमों के साथ जीना आ जाऐ गलियां बदल जाऐं, लोगों का बरताव बदल जाऐ जिसमे पुरानी दिल्ली भी बदलती दिल्ली का ही हिस्सा लगे यहां भी लोगो के साथ बदलाव चले ।
लेकिन हम इस पीढ़ी मे भी वैसे ही जीते है जैसे हमारे बड़ो मे पुरानी दिल्ली को जिया है वो मज़ा जो उन्हें सुनने मे आता है उनके मज़े के आगे अपना मज़ा कहीं फीका सा लगता है और उसी मज़े को और मज़ेदार करने की कोशिश मे लोग और जगह दोनों जीये चले जा रहे हैं मस्ती में।
सैफू.
Labels: संवाद
चैलेंज
"भाई वसीम दो रुपय के सिक्के देना ।"
गैम की दुकान मे दखिल होने का यही तरीका था मेरा। यहां के वीड़ियो पार्लर में गैमों की भरमार है यहां तकरीबन 20 गैम की मशीने है जिसमें से 2 गैम एसे है जिसमें 999 तारीके के गैम खेल सकते है। पर मेरा मनपसन्द गैम एक ऐसा गैम है जिसमे दो लोग एक साथ चेलेंज कर सकते है और यही चेलेंज हमें जीतने और हारने जैसी प्रक्रिया मे रखता है ।
मुझ पर घर वालों का डंडा भी हैवी होने लगा था । रोज़ घर वालों की सुनता पर मानता अपने दिल की । रोज़-रोज़ दो-दो घंटो के लिये गायब रहता और जब घर वाले पुछते "कहा था ?"
तो बतोलेबाज़ी दे कर घुमा देता । पर डर लगता उनके होने के एहसास से जिसमे मे शामिल भी होने से कतराता था ।
एसी जगहें जिसमे कुछ करने की, कुछ सीखने की प्रक्रिया मे खोने के एहसास को लोग या समाज़ कुछ अलग बोली या नज़र से सम्बोधित करते है । पर वो समाज वो लोग दरासल में हमारे घर वाले ही होते है, जो इस समझ को बनाए बैठे हैं ।
: कि मेरा बच्चा सीखने जा भी रहा है तो गैम जिसका सीधा मतलब खेल होता है, किस के मां-बाप चाहते है कि उनका बच्चा पढ़ाई की उम्र में अपना ज्यादातर वक्त खेल मे लगाए...
लेकिन खेल ही तो है जो सबसे पहले घर वाले बच्चे को सिखाते है और बाद मे उसी से दूर भगाने की कोशिश...?
मेरा खुद से खेल को सीखना और मेरे घर वालों का किसी खेल को सीखाना दोनों किस संदर्भ मे अलग-अलग दिशाऐं देते हैं ?
सोच और गलत धारणा के साथ बच्चे कुछ सीखने के साथ-साथ कई अलग चीज़े भी सीख जाते है जिनकी उन्हे उम्मीद भी नही होती ।
पर मेरे साथ एसा नही था ! घर वाले कहते-कहते थक जाते मगर मैं बाज़ नही आता, उनके मना करने के बाद भी मैं गैम खेलने रोज़ पहुच जाता और उनके आने पर उस दुकान के किसी कौने मे छिप जाता... अब तो इतना हो गया था कि मेरे घर वाले जैसे ही आते तो गैम का मालिक( भाई वसीम )मुझे इशारे से पहले ही बता देते और कभी-कभी तो मम्मी को बाहर से ही मना कर देते कि "ऐबी तम्हारा बेटा यहां नही है ।"
अब मेरा घर से गैम और गैम से घर आना आसान हो गया था ।
जब कभी मम्मी पूछती : तू गैम मे से आया है ना ? तो मैं मना कर देता और साथ मे ये भी कहता
: भाई वसीम से पूछ लो जाकर अगर मैं झूट बोल रहा हूँ तो ?
वो मेरे ये बोलने से कभी भी वहां पुछने नही जाती थी ना जाने क्यू ?
वो मेरी बातों का यकिन था या कुछ और मुझे नही पता... पर उन्हे इतना तो मालूम था कि मै रोज़ गैम खेलने जाता हू ।
अब तो मम्मी ने भी मुझसे रोज़-रोज़ पुछना बन्द कर दिया था । पर कभी-कभी बाई-चांस पूछ लेती थी तो उनका पूछना और मेरा जा कर भी मना कर देना चालता रहता । मैं अपने गैम से खुश था इसलिए मै बतोलेबाज़ी का उस्ताद बन गया और घर वालो को घुमाता रहता अपनी बातों से ।
इस बीच मेरे गैम में काफी सुधार आ गया था और मेने गैम खेलने के काफी तरीकों को अपने ज़हन मे बिठा लिया था, मैं अपने बराबर या अपने हमउम्र लड़को का भी गैम ओवर कर दिया करता था , एक सिक्क़े मे रानी मिलाना और स्कोर बनाना मेरे दाए हाथ का खेल था। पर अब भी मैं भाई लईक से चेलेंज करने से डरता था, उनकी मोज़ूदगी में मैं अपने आप को कहीं छोटा सा महसुस करता था ।
उनके साथ ना खेलना मेरे लिए एक पहेली सा बन गया था जिसे समझ पाना मुशकिल सा लगता था। एक कोने मे खड़े होकर चुपचाप उनके गेम को देखता रहता था । यह देखना भी मुझे काफी कुछ सिखाता । इसी से मैं अनेक सीखने-सिखाने की छुआन को उस कोने मे खड़ा सीखता रहता ।
एक दिन भाई वसीम ने कह ही दिया कि : कब तक खड़ा रहेगा ? कभी तो खेलेगा ही ?
" चल सिक्का डाल ।" उन्होने यह कहकर मेरा सिक्का उस गैम मे डालवा दिया । मैं खुश नही था मुझे पता था कि मेरा सिक्का बेकार गया । यह अभी दो मिनट मे मेरा गेम ऑवर करके भागा देंगे मुझे। इनके सामने मेरा तो गेम ऑवर होना तो तय है । इन्ही को तो देख कर सिखा हु भाला केसे हरा पाऊंगा इन्है ? अब सिक्का डाल ही दिया है तो खेलना ही पड़ेगा ।
उस जगह थोड़ा चेलेंज स्वीकारा लिया मैंने और उनके साथ खेलने लगा ।
वो मेरे साथ मज़ाक से खेल रहे थे उनका उनका कहना था की मेरे तीन पिल्यरों को एक से ही मार देंगे । इसलिए वो मुझसे मज़ाक से खेल रहे थे । उनके मज़ाक के खेल से भी मैं जी-तोड़ मेहनत करके लड़ रहा था । पता नही मुझसे खेला क्यो नही जा रहा था। क्या ये सब उनका डर था या गैम ऑवर होने का ?
उनके दो पिल्यर मर गये थे और मेरा एक । उन्होने मेरा दूसरा पिल्यर भी बच्चे की तरह मार दिया । पर तीसरे पिल्यर से मैंने उनका पिल्यर मार दिया । मैं मन ही मन खुश था उस समय मैंने उनसे दूसरा सिक्का डालने को मना कर दिया ।
वो भी हसी मज़ाक करते हुऐ आपने घर चल दिये । मन ही मन मैं खुशी से भरा था की भाई लईक को घर चलता किया है मैंने। इस बात को मैं हफ्ते भर तक गाता रहा था भाई वसीम की दुकान में ।
मनोज.
Labels: महफिलों के बीच से...
"मीना बाज़ार"
पुरानी दिल्ली की छोटी-बड़ी मंडलियों को समेट कर अपनी पहचान को पक्का करती ये ठिऐ नुमा दुकान मीना बाज़ार की सीढ़ियों पर एक ऐसा माहौल तैयार करती है जिसमे एक को देख एक मस्ती मज़ाक, जोरा-जोरी, लड़ाई-झगड़े से माहौल को भारी-भरकम बनाऐ रखते है। जो देखने-सुनने, उठने-बेठने मे बड़ी ही मज़ेदार जगह लगती है,
पर ये मज़ेदारी का एहसास कहां से आता है?
क्या जिस माहौल मे हमारा उठना-बेठना नही होता वो मज़ेदार या अदभुत होता है?
या हम ही से बनी जगह का एहसास जगह को खास बना देता है?
लोगों की शिरकत और एक ऐसे टाईम में दुकान का चलना जिस टाईम में लोग ढूढ़ते है ऐसी जगहों को जिसमे बैठ रात कट जाऐ, जिसमे रात का अंधेरा मन को सकून दे।
अलग-अलग छवियों, माहौलों और बातचीत से बनाऐ रखती है ये जगह अपने आप को दूसरों से अलग।
सैफू.
Labels: महफिलों के बीच से...
छवि, जगह और सोच.
छवि...
जिसकी अपनी एक पहचान, नाम और अदा हो, जिसके होने और न होने से जगह और सोच को बोलने के तरीके मिलते हैं।
वो तरीके जो छवि की पहचान से जोड़ कर समाज में रखे जाते हैं कभी नसीहत तो कभी सीखने-सिखाने की बोलियों में...
छवि वो भारी शब्द है जो माहौल की रूपरेखा पर अपनी छाप छोड़ बयां करने और देखने के नज़रिये को बदलने की क्षमता रखता है जिसमें कभी आप बदले-बदले से लगते हो तो कभी आपकी शख्सियत और स्भाव....
जगह...
जो फैलते, सिकुड़ते आकार में नाप-तोल करके बोली या देखी जाती है, जिसके बया पर उसको किसी नाम से पुकारा जाता है... और वो बोले जाने वाले नाम जगह में अपने मतलब को तलाशते फिरते हैं किसी की आँखों मे, किसी की बातों में तो कभी वहां भटकते चहरों में कि आखिर ये बक़चौदियां क़्लब है कहां?
ये नाम किसी कैरम क़्लब को वहां के बड़बोलेपन की वज़ह से दिया गया है। जगह का मालिक इस जगह को नाम देता है फैंसी क़्लब पर वहां की रिज़मर्रा मे शरीक होने वालों का यहां कहना है कि किसी से भी पूछ लैना बक़चौदियां क़्लब कहां है? तो वो सीधा यही का पता देगा।
जगह और नज़रियें दोनों एक दूसरे से लड़ते नज़र आते हैं कभी देखा-देखी मे तो कभी कहा-सुनी में। जिसमें नज़रियां बदले या न बदले जगह बिना किसी बदलाव के नामों से बनी पहचान को बदलती रहती हैं।
सोच...
बोलने और संभलकर बोलने के बीच की समझ जो कि सोचकर बोलने की भाषा को तैयार करती है। और वही सोचकर बोलना ज़हन में जगह और छवियों को गाढ़ा करने के माद्दे को और गहरा कर देता है जिसमें हम कभी खोए-खोए से कहलाते हैं तो कभी अपने मे मगन से।
पर यही सोच शख्सियतों को जगह भी देती है तो कभी अपने में न होने का एहसास भी दिलाती है।...
"नंगा नहाएगा क्या और निचौड़ेगा क्या?"
ऐसे मुहावरे किसी सोच मे बहते है जिसमें हम अपनी बोली लाईनों में किस सोच को किसी की ओर फैंकते हैं उसको समझ या समझापाना कभी साफ तो कभी धुंधला सा लगता है।
सैफू.
Labels: संवाद
चाहतों से बनी जगह
जब एक दूसरे की सांस से जगह हमेशा ज़िंदा रहने का मुकाम बना लेती है तो उस जगह का दम तोड़ना या कुछ घंटों के लिए जिंदा होने की मौज़ूदगी में रहना मुश्किल हो जाता है।
उसके बीच उस जगह को कौन उस जगह के होने की मौजूदगी में रखता है, चबूतरे के मालिक को कोई लैना देना नहीं।
अब वहां कोई रात के 2 बज़े तक चाय का ठिया लगाए या अण्डे-पराठे की रेड़ी। वहां लगने वाली भीड़ उस जगह के आकर्षण के आकार को और फैलाती रहती है।
आप यहां एक दूसरे को देखकर उसके जैसा रंग अपना सकते हो, क्योंकि वो जगह ही बनी हुई है एक दूसरे के रंग से, कोई अपना रंग लेकर आता है तो कोई अपना रंग भूल किसी और के रंग में रंग जाता है। कोई अपनी जगह में रहने की हिदायत देता नज़र आता है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी करे उनका मानना है कि जैसा करेगा वैसा भुकतेगा।
हंसी-मज़ाक करते रहना और 5-10 रू के पीछे इन जगहों के हसीन पलों को छोड़ना कोई नहीं चाहता। पर ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं ये नशा है, जुआ है अपनी जिंदगी के साथ, अपने वक्त के साथ।
वो चाहते हैं कि वो समय की कदर करें और अपना समय बरबाद करने से बहतर किसी काम में लगाऐं, पर उस जगह में आ रहे लोग इन बातों से कहां प्रभावित होने वाले, वो जानते हैं तो बस...
"कुछ पल की जिंदगी है, आज है कल नहीं तो कुछ पल अपने लिए ही सही" जिसमें मैं हूँ, मेरे दोस्त हों, मेरा अंदाज़ हो, हमारी हँसी हो, एक-दूसरे का सुनना सुनाना हो, कभी सलाह मशवरा हो तो कभी-कभी बस यूंही आना हो।
पर कुछ पल हों जो अपने काम से परे हों, घर-परिवार से परे हो, करीयर की टेंशन से परे हो और उसमें हो वो जो मज़ा भी दे और खुशी भी, जिसमें बार-बार जाना कभी बोरियत न बने, बने तो बस दुबारा बार-बार जाने का नशा, रोज़ अलग मज़े का नशा।
जिसको में उस जगह के आकर्षण के रूप में देखू तो कभी ज़िद या आदत में।
यहां कौन कहां से आता है? क्या करके आता है? कब आता है? और कब तक जाता है?
ये न तो किसी को जानने की जरूरत है और न ही किसी को बताने की...
यहां बहुत कुछ अपनी मर्ज़ी पर निर्भर होता है और बहुत कुछ नहीं भी।
सैफू.
Labels: महफिलों के बीच से... , शिरकत
बनाने से बनने तक...
वहां से होकर गुज़र जाने वाले क्या समझते हैं उस जगह को, वहा बैठे लोगों को, उनकी सोच से परे ये जगह आपके सामने हमेशा वेलकम ही बोलती नज़र आती है। कभी वहां की आँखों से तो कभी वहां की बातों से...
इस जगह से कभी गालियाँ बाहर आती है तो कभी उनका बचपन या बचपना, कभी किसी का बड़ा होना बाहर आता है तो कभी किसी का सीख का गुरूर....
सबके बनने या बढ़ने का दायेरा चाहे कितना ही क्यों न हो वो निकलता है उसी गेट से जहां से वो जगह मे शामिल हुआ था।
हर कोई अपने लिए उस चार दिवारी में कुछ न कुछ तैयार ही करता मिलता और जब बाहर आता लोगों या महफिलों में उतरता तो एक पहचान, नाम या अंदाज़ मे, जिससे कभी उसे नवाज़ा भी जाता तो कभी चिड़ाया भी।
कभी वही नाम और अंदाज़ उसकी कमाई का ज़रिया बन जाता तो कभी मज़ाक की शक़्ल मे उसे खड़ा कर उसके नाम और अंदाज़ से मज़ाकिया माहौल तैयार किया जाता।
बनने वाला भी उन्ही में से कोई एक होता और बनाने वाला भी।
सैफू.
घूमती समझ.
आकर्षण वाली जगह का एक मापदण्ड़ हम अपने साथ लिए चलते हैं जिसे हम कभी, "टाईम पास है","वक्त गुज़ार रहा हूँ "
ऐसे शब्दों के नीचे दबाकर रख देते हैं। जो हमारी एक जरुरत बन जाती है। जब कोई जगह हमें अपनी ओर आकर्षित करती है तो कभी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं या नकारकर कोहरे की धुंध में खो जाने के लिए छोड़ देते हैं।
पर हो रहे आकर्षण को हम कैसे अपने आप में समा लेते हैं यह एक सवाल जवाब के साथ बन जाता है जिसे हम अपने ही शब्दों मे खेल जाते हैं।
हम रोजर्मरा की रुटीन में कितने ही आकर्षणों को अपनाते हैं?
यह भी हमारा ही स्वार्थ तय करता है। एक जगह हमें दूसरी जगह से आकर्षित होने की प्रेणना देती है, जिसे हम साथ लिए और आकर्षणों को खोजते रहते हैं।
ऐसे ही मेरा एक दोस्त जो अकसर दूसरे घरों की सज़ावट को इक्ठठा कर अपनी काल्पनिक घर की तैयारी में लगा रहता है। वो अपने घर का आकर्षण दिखाने के लिए चीज़ों को देखता और पसन्द करता है।
*उसके लिए अपना और उसका आकर्षण क्या मायने रखता है?
*पर अकसर लड़ाइ होती है कि जगह की हमसे मांग क्या है?
*अगर हमें कोइ चीज़ पसन्द आती है तो क्या वो हमारा आकर्षण है?
*या किसी जगह में समय देना वो हमारा आकर्षण है?
*जगह मांगती क्या है? आपका वक्त या आपकी पसन्द ?
*आपके देखने के तरीके को झुटलाना या बनावटी आकर्षण को आपकी नज़रों में कैसे उतारा जाऐ उसकी एक समझ?
कभी लगता है कि किसी जगह में हो रही क्रिया जो काफी निम्न गति में अपने आकर्षण को एक व्यावस्थित रुप में लाने की कोशिश में लागी दिखाई देती है, जो कभी खत्म नहीं होती।
इस क्रिया में चीज़ें जुड़ती रहती हैं जो उस जगह के आकर्षण का केन्द्र बिन्दू बन उभरती है।
मनोज.
शरीर...
जिम की तस्वीर को अगर देखा जाए तो उसका सामान ओर आकर्षित शरीर ही उसकी नज़र को और गाढ़ा करता है।
जो कई तरीकों से अपने आकर्षण को बयां करते फिरते हैं, कभी दोस्तों की मंडलियों में तो कभी देखा-देखी में जिसमें बनने-बनाने की बातें जो सामने वाले से होकर आपके अपने शरीर की बनावट तक आकर रूक जाती हैं। कि
"काश मैं भी ऐसा होता?“
अगर मैं भी जिम जाने लगू तो कैसा लगूंगा?
मेरे शरीर के साथ-साथ मेरे कपड़े पहनने के तरीकों में कितना फर्क आ जाएगा? ऐसे कितने ही सपने जो कल्पना की उड़ान में हमको हमारा जिम से जुड़ा आने वाला कल दिखाता है। ऐसी बहुत सी बातें या अपने आप को देखने की नज़र का बदलना दिमाग में जिम की तस्वीर को और गाढ़ा कर देता है और फिर एक ज़िद्द या अच्छा शरीर पाने की तमन्ना हमको जिम की ओर खींच लेती है।
जिसके खिंचाव के दोरान ऐसे बहुत से शरीर, बहुत सी बातें आपकी उत्सुक़्ता को और बढ़ा देती है जिसमे हम कई पड़ावों को अपना लेते हैं सिर्फ़ अपने मैं के लिए और वो पड़ाव कभी जिम को लेकर खर्च होता है तो कभी उसके लिए टाइम निकालना या दोस्तों से कटना। और यही मैं अपने आपसे एक आस लगा बैठता है, पतले हाथों को डोलों में तबदील होते हुए, पतले बदन को चौड़ा सीना बनते हुए देखना चाहता है
जिसमें मैं भी सामने वाले के लिए एक आकर्षण बनके निकलू और ओरों को एक नज़र दूं कि "ऐसा होता है शरीर"
सैफू.
कोई पहचान
चप्पलों की घिसावट के साथ हम अपनी दूरीयों को नापते चले जाते है। नज़रों से नज़रों को मिलाते फिर चुराते अपने उस मुकाम को पाने की कोशिश में रहते हैं जो कभी हमारा था ही नही। फिर मिलते है समय के उन टाईम टेबल से जो एक निर्धारिता मे बंधा है।
अपनी ही तरह की आज़ादी को पाने की होड़ लोगों को कहीं से भी खेंच लाती है। लोग दूरीया नापकर अपने नेटवर्क को बड़ाने के लिए कही से भी भागे चले आते है इन अनमोल जगहों की तलाश में।
वो अपना समय उन लोगों के नाम कर देते हैं। जो चैलेंज की एक बनी हुई प्रक्रिया के साथ मिलते है। लोग चाकू की तेज़ धार लिए आपको हराने के तरीके को पैना करते और अपने गैम मे माहिर होने की बुनाई में लगे रहते है।
उस बुनाई की हर एक गाठ रोज़ एक नए मेम्बर की तलाश को चारों ओर फैला देती है।
कभी-कभी मंडलियों के बिगड़ने की बातों को भी यहां का मुद्दा बना लेते है "कहां गया तुम्हारा चौथा पार्टनर" "दिखाई नही दे रहा, काफी दिन हुए उसे देखे हुए" अगर वो सही है तो ठीक, नही तो उसके बारे में ही उस जगह में उसकी चर्चा होने लगती।
मुद्दा कुछ एसा होता जो लोगों को या तो सिरियस या फिर माज़ाकिया तौर पर ले जाता। बगल की सीटो पर बैठे लोग अपनी दूरीयों के तय किये हुए इतने समय से बने दायरों को फैलाने और बने नेटवर्क खत्म न हो जाए इसी डर में रहते हैं। और बुनते रहते है अपनी बुनाई को उस क्लब में।
मनोज...
शख़्सीयत
एक ऐसी छवि जो बाज़ार में तो कभी गलियों में घुमक़्कड़ों की तरह जिंदगी के रंगों को जीते हैं और हमारे आस-पास भी ऐसे कई शख्स हैं जो हमें बहुत से नुक्कड़, चौराहों और गलियों में गाना गाते, अपने आपसे बातें करते, चीखते-चिल्लाते और उन बच्चों को गालियाँ बकते नज़र आते हैं - जो उन्हें पागल-पागल कहकर चिड़ाते हैं।
न वो ये साबित कर सकते हैं कि वो पागल नहीं हैं और न वो कहते की जुबान रोक सकते हैं वो बस उनसे दूर अपने आपको कहीं समेटना चाहते हैं, कहीं किसी कोने में। जो कौना समाज उन्हे नहीं देता और अगर देता भी है तो एक चुप्पी के साथ... जिसमें न उनको सुनने वाले कान होते हैं और न ही बत से बत्तर हालात में देखने वाली आँखें, न रहने को छत और न पहन्ने को साफ कपड़े, कोइ ढ़ैर सारे लिहाफ-बिसतरों मे लिपटा दिखाई पड़ता है, मौसम चाहे कैसा भी हो उसे न गर्मी लगती है और न सर्दी...
तो कोई सिर्फ़ चार पट्टीयों मे लिपटा सड़को पर घूमता रहता है।
उसके लिए न शर्म है और न लोगों के ताने कि "तूने पहन क्या रखा है?"
और अपने नंगे शरीर को पूरे बाज़ार में लिए फिरता है न कोई उसको दो कपड़े पहनाने वाला है और न कोई ये कहने वाला कि "दो कपड़े तो पहन ले"
कोई-कोई तो इस कदर चीख़ता हुआ दिखता है कि मानो उसको कोई सरे-आम सड़क पर हंटरों से मार रहा हो पर उसको मारने वाला कोइ नहीं होता वो अपने आप उस चोट को महसूस करता और जोर-जोर से चिल्लाता, अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालता, न जाने वो जोर और वो कड़कपन उसकी आवाज़ में कहां से आता है?
कुछ ही दिन पहले की बात है एक शख्स दिल्ली गैट से पहले पड़ने वाले तिराहे चौक के एक साइड में बैठा अपने आप में बड़बड़ा सा रहा था। मैं उसे देख वहीं एक जनरल स्टोर पर रुक गया और कुछ खरीदने लगा। बार-बार मेरी नज़रें उसे देखने और मेरे कान उसे सुनने को बेचेन से हो गए थे। दुकानदार ने पूछा भी कि ....
क्या लेना है ?
मेरी नज़रें एक पल उसकी तरफ मुड़ी और वापस उसको देखने लगी और होटों से आवाज़ निकली " ब्लू पेन देदो कोई सा " अपने हाथों को कान पर लगाए मोबाइल की कल्पना ने उसे अंधा बना दिया था कि उसके पास मोबाइल है।
मैं उसे ही देख रहा था।
वो : " हैलो हां मजिस्टेड साहब हां मेरी कल की फ्लाइट है, मैं कल नहीं आ सकता "...
" हाँ हाँ वो मैं अभी एक जरूरी मीटींग में हुँ मैं कल आउंगा "...
" हैलो शुकला साहब मेरी अमेरीका का टीकट कटवा दो, मैं कल आपसे मिलनें आउंगा "...
ऐसी कई सारी बातों से वो अपने आपको एक रहीस आदमी की छवि में उतारता और उसे भूल जाता जो दुनियां देख रही हैं पर वो नहीं कि वो मैले-कुचेले कपड़ों में, बिना जूतों के मोज़ों में, कुड़े के ढ़ैर के पास बैठा, शक़्ल पर बेवारसी और होंटों से निकलती बनावटी हँसी और शब्द।......
न जाने वो हर काम कल पर क्यों टाल रहा था और कल की सोच की वजह से ही शायद वहां पड़ा था। रोज़ एक नया कल पर आज की कोई छवि नही।
खैर मैं दुकानदार को बिना कुछ दिये और बिना कुछ लिये ही वहां से आगे बड़ गया। ये सोचता हुआ कि " सारे उलटे-सीधे दिल्ली में ही पड़े हैं। " उसे देखने के बाद और बाद में उसे सोचने पर मुझे मन ही मन हँसी आती रही कि
हालात चाहे कैसे भी हों पर उसका सपना छोटा नही था।
सैफू.
Labels: देखा-देखी , यादों की दुनियां...
12:45 चाय की दुकान...
चार लोग दो-दो के ग्रुप में आमने-सामने बैठे हैं लकड़ी की टेबल पर। उसके ऊपर का कलर चाय वाले ने अपने पोछे के कपड़े में सोख लिया है।
पूरे भरे हुए चार गिलास पानी उनके स्वागत पर उन्हें दिये गए हैं। चारों 35 से 40 तक की उम्र तक के होंगे। सबने सर्दियों के मुताबिक गर्म कपड़े पहन रखे हैं। उनमें से एक के बाल अनुभव की रेंज में आकर पक चुके हैं। बातों का सिलसिला उनके स्वागत से पहले ही श्री गणेश हो चुका है।
पहला आदमी : (बालों का रंग सफ़ेद होने के हिसाब से सबका पंच लगा रहा है) थोड़े गम्भीर स्वर में बोला, "आज जुनेद का एक्सीडेंट हो गया।"
दूसरा आदमी : (अपनी पतली काया और काली चमड़ी के साथ)
चौंकते हुए पूछा, "कब?”
पहला आदमी : हल्के स्वार में बोला। "आज सुबह।"
(बोलने का तरीका और चहरे के भाव से लग रहा था कि जैसे किसी मछुआरे की नौका सम्रुद्र में डूब रही हो और वो बेचारा दुखी किनारे से सब देख रहा हो)
दूसरा आदमी : "वो कल ही रास्ते में मुझसे दुआ-सलाम करता जा रहा था।"
(यह उस मछुआरे को सहानुभूति देकर दुख की छाया से बाहर निकालने की कोशिश में लग रहा है।)
पहला आदमी : "ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, बाईक पर था। अभी तो निकलवाई थी उसने। मैं तो उसे देख भी
नहीं पाया"
(मानो जैसे पूरा दृष्य उसकी आँखों के सामने फिर रिवाइन्ड हो कर आ गया हो)
टककक... चाय के गिलास टेबल पर आ गये और वो भी अपनी चिंतन से बाहर आ गये। थोड़ी देर सब शांत रहे मानों जैसे मोन व्रत हो और फिर चाय पीने लगे। माहौल पता नहीं कहाँ गुम था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि "मैं कहां हुँ?“
मनोज.
Labels: महफिलों के बीच से...
छत्ता लाल मिया " जिम "
ये एक लोकल जिम है जिसकी बनावट कुछ खास नहीं है। पुरानी दिल्ली में ऐसे कई जिम गलियों-चौराहों पर चलते हैं जो अपनी बनावट से ज्यादा उसमें एक्सर्साएज़ कर रहे बन्दों पर गोर करते हैं वैसे यहां के आस पास के सभी जिम 60-70 गज की लम्बाई-चौड़ाई में ही बने हुए हैं जिसमें 100 से 150 बन्दे रोज़ के आते हैं, बाकाएदा उनकी रजिस्टर में एंटरी होती है और महीना आते ही याद दिला दिया जाता है कि
"भाइ आपका महिना हो चुका है" !
जिम अकसर दो टाइमिंग में चलते हैं सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 10, यहां लड़कों में जिम का इतना शौक़ हैं कि सुबह-शाम ये दोनों टाइम ही भरा हुआ मिलता है।
यहां का अपना ही एक माहौल होता है जो हमें बाहर की एक समझ देता है कि लोग अब लोगों को कैसा देखना चाहते हैं।
मैं अपने आप में कैसा दिखता हूं और क्या बनना चाहता हूं? ये सवाल अपने आने वाले कल को लेकर ही होता है पर सिर्फ दिखावे में जो दिखता है उसके लिए। कुछ बनने से पहले हम उस दुनियां की कल्पना में खोये रहते हैं जो हमको उस बहाव में तैरने का एहसास देता है।
दोस्तों के बीच खड़े होने का तरीका और सड़क या बाज़ार में घुमने के स्टाइल की एक हवा सी गुज़रती है दिमाग में जिसके झोके हमको जिम से बांधे रखती है। फिर ख्याल आता है कि आप उस जगह में अकेले नहीं हो वहां आप जैसे शुरूआती बहुत हैं, जो अपने से और उस जगह से एक दिलचस्पी से जुड़े हैं।
जिम की बनावट और यहां की सजावट हमको एक ऐसे आकर्षण की ओर ले जाता है जो आप चाहते हो। इसका मैन मुद्दा है अपकी चाहत को समेट कर लाना और उत्साहित करना।
फिल्मी हीरो के फोटो लगाना, सलमान खान बिना शर्ट के, जोहन इबराहम की चेस्ट, शाहरूख के सिक्स पैक, उदय चौपड़ा के डोले और बाक़ी होलीवूड की फोटो, आर-नोल्ड वगैरह...
इन सब शख्सियतों को देखने पर देखने वाले को क्या उत्सुकता मिलती है ये समझ हर जिम के पास होती है वो अच्छे से अच्छा फोटो लगाता है, क्योंकि ये सब शख्सियतें ही उसके जिम का आकर्षण हैं, इतना सब देखने और अपने साथ एक्सर्साइज़ कर रहे छोटे-बड़ों से इतना तो पता चल ही जाता है कि शुरूआत क्या है और आगे क्या होगा।
बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमको इसका अन्त समझाते हैं कोई रोककर तो कोई सलाह मशवरे में। इस जगह आपसी बातचीत का एक अलग ही रोमांच है जो बाकी सब जगहों से अलग है
जिसमें हमउम्र होने की वजह से अपनी बात को कही भी रखने में कोई झिझक नहीं होती, जिसमें "धिरे से बोल"
ये लाइन कहीं खोई सी लगती है।
जिम में नए चहरों को देखकर लगता है कि इनके भी कई सपने होंगे इस जगह से जुड़ी कितनी ही उम्मीदें और बातें होंगी, जिसको पूरा करने की आस में ये या तो सफल हो जाएगें या फिर कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय अएगा कि ये भी मेरी तरह जिम आना छोड़ कर, उसके सपनों और यादों में ही घूमते रहेगें।
सैफू.
Labels: देखा-देखी , महफिलों के बीच से...
" आर्कषण "
जो हर पल अलग-अलग रूप में उस जगह में बहता रहता है जो न सिर्फ़ मेरा है और न सिर्फ़ तुम्हारा...
वो अकर्षण है किसी की शुरूआत का, किसी की आदतों को बरदाश करने का, सुनकर अनसुना करने का और बार-बार भगाने के बाद भी रोज़ वहां लगने वाली लड़कों की टोलियों का।
यहां लोगों ने इन जगहों को अपने तरीके से देखने की आदत डाल ली है और बना लिया है वो नज़रियां जिसमे बोलने और सुनने वाले सिर्फ़ वो हैं जिनसे ये जगह पनपने के उस ताव में है।
इसमे सदा से अच्छे और बुरे की बहस रही है जिसमे कोई पास तो कोई फैल रहा है और पास फैल की भाषा में इन जगहों को उतारने वाले और कोइ नहीं इसी जगह के वो लोग होते हैं, जो इस जगह के आस-पास को सोच कर, लहज़े-तमीज़ को सोच कर, अपने-पराए की परख पर, नऐ-पुराने अड्डे की पहचान को मुद्दा बना कर और इलाके की शिकाएतों या फरमाइशों पर इस को बना या बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
यहां हर तरीके के लोग आते हैं। कोई गुटखा खाता हुआ तो कभी-कभी पूरी दुकान में सिगरेट का धुआ ही छाया रहता है।
यहां गालियां भी बकी जाती हैं और गलियों को सहा भी जाता है और हर तरीके का मज़ाक भी किया जाना लाज़मी सी बात है। यहां गर्म खून के लोग भी बहुत आते है जिनके मुँह मे गुटखा, नाक से बीड़ी का धूआ और मन में हमेशा मारने-मरने की बातें भरी रहती हैं।
छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे की खिचाई भी और जुगलबंदी में अपनी बात से सामने वाले को चुप कराने की तरकीब भी, जिसमें एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा जाता कि कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा?
सैफू.
Delhi-06
दिल्ली 06 उन पहलूओं से बना हुआ है जो पल-पल हर एक नज़र में आपको एक नई भाषा देता है माहौल को बयां करने की, जिसमें टाइम-टेबल और सिमटते माहौल में भी एक-दूसरे को वो खुशी बांटते चहरें मिल जाते हैं जो इस दौर में कहीं गुम से लगते हैं।
पल-पल की कीमत होती है ये कहता है हमारा समाज, घर-परिवार, हमारा खुद पर हमारा खुद भी हमसे कुछ चाहता है और उसी चाहत में लिपटे लोग अपने खुद को महफिलों मे उतार आ मिलते हैं जिल्ली-06 की उन जगहों में जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हर जगह अपना समाज खुद तैयार करती है और दिल्ली-06 का अपना खुद का समाज है तभी इसे पुरानी ज़ुबानों से लेकर आज तक पुरानी दिल्ली ही कहा जाता है जिसमें कहने-सुनने वालों की भाषा भी वही मांगता है जो उनका खुद चाहता है।
लोगों की चाहत से जगहों का बनना पुरानी दिल्ली की ख़ासियत है। जिसमें हर एक जगह अपने होने पर गर्व करती है और वहां से निकलती आवाज़े कहती हैं "हम अपने मालिक खुद हैं, कोई ओर कौन होता है हमें रोकने वाला" जिसमें कभी बड़े-बूड़े अपनी बहकती आवाज़ में कहते नज़र आते हैं
"पुरानी दिल्ली, दिल्ली का वो कोना है, जो दिल्ली को पहचान देता है।"
"यहां जैसा बाज़ार और महफिलें ओर कहां?”
"दिल्ली बदल रही है पर पुरानी दिल्ली जो थी वो है और अल्लाह ने चाहा तो ऐसी ही रहेगी"
तो कभी घूमते चहरे, आवाज़ें लगाते बैझिझक लोग माहौल को बदलाव के भाव में उतारते से लगते हैं। जिसमें कभी चाय के ठिए शामिल हो जाते हैं तो कभी रेढ़ियों पर लगा फल-फ्रूट का मेला जो रोज़ की रोनक है। कभी ओरों की चाहत को अपनी दुकान मे सजा लोग खेंचते नज़र आते हैं लोगों को तो कभी लड़ाई झगड़ो से शांत सी दिखती गलियाँ, चौराहें और बाज़ार।
बाहर दिखता है वो जो सुनने में आता है पर इसके अंदर अपनी चाहतों के दरवाजों को कोई खोले बैठा है।
हर एक गली, हर एक मोड़ और चौराहा उसमें रहने वालों की मांग और चाहत की समझ से बनाए बैठा है वो महकमें जो टाइम-पास जैसी भाषा में अपने को वहां जमाए हुए हैं जिसमें उतरकर कई लोग जीते है, जिसमें जगह और लोग एक दूसरे की रोज़मर्रा को सजाते से लगते हैं।
कैरम क़्लब, चाय की दुकानें और ठिए, वीडियो गेम, जिम ऐसे कई महकमें अपनी अपनी परिभाषा लिए पुरानी दिल्ली मे उसी के टाइम-टेबल के अनुसार अपनी व्यवस्था और बनावट में हैं।
सैफू.
इस बनने की शुरूआत कैसे हुई?
 राहों से अपनी पसन्द की चिज़ों को चुनकर इकठ्ठा करना और अपना घर तैयार करना।
राहों से अपनी पसन्द की चिज़ों को चुनकर इकठ्ठा करना और अपना घर तैयार करना।
यही तरीका है केरम क्लब के बनने का जिसमें क्लब का मालिक अपनी मर्ज़ी से क्लब को किसी तैय्यारी में सजाता है।
पसन्द न पसन्द आर्कषण के मुताबिक माहौलों को देखकर तैयार करता। जहाँ माहौल टाईम-पास होने का या करने का समय नहीं देता वहाँ केरम जैसे टाईम-पास खेलों को जगह मिल जाती है। जिसमें महफिल बनती, जुड़ती, संवर कर अपना खेल पैना करती नज़र आती है। खेल को पैना करना और उस खेल को बनाए रखने की होड़ में महफिलें इन जगहों को अपनी रोज़मर्रा में जोड़ लेती है।
एक केरम क्लब अपनी लम्बाई-चौड़ाई को जब तक लोगों की मौजूदगी से भर नहीं लेता तब तक कैरम क्लब खाली सा लगता है पर जब भीड़ होती है तो जगह का मालिक अपनी बनावटी दुनिया से खुश हो जाता है।
दो कैरम बोर्डो का यह महकमा सिमटता और अपने में सबको समेटता सा लगता है।
पर सब भूल लोग अपने हुनर को दिखाने में लग जाते हैं जिसमें से अनेक परछाईयाँ अपना प्रतिबिम्ब छोड़ चली जाती हैं। जिनकी छोड़ी गई धूल हर कोने में लगी दिखती है। वो कोना उनकी याद के साथ तैयार हो कर कुछ पलों को याद करने का रुप बन जाता है।
हर किसी के पास अपने समय का चक़्कर अपने हाथ की उंगलियों पर गढ़ा है। जिसमें से हर उंगली अपनी एक प्रतिक्रिया में मशरुफ़ नज़र आती है। जिसके खाली स्पेस में केरम जेसा खेल अपना भराव बनाए हुए है।
Labels: देखा-देखी , महफिलों के बीच से...
जगहें ...
कई जगहें हमें अपने आप मे सिमटने और बहने के बहाने देती हैं, वो बहाने जो कभी हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं तो कभी रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी एक जगह बना लेते हैं। और उनका ये जगह बनाना हमें उस पर सोचने और बोलने के कई तरीके दे जाते हैं, वो तरीके जो कभी हम दोस्तों की मण्डलियों में बोलते नज़र आते हैं तो कभी किताबों मे लिखते।
क्योंकि हर जगह पहले वक़्त मांगती है फिर आपकी आदत और फिर उसके तरीकों की एक समझ कि यहां कब, कैसे और क्यूं?
और वहीं समझ हमारे शब्दों में उस जगह के लिए एक शब्द और जोड़ देती है, कभी
वाह-वाह में तो कभी टाइम-पास में कभी मस्ती में तो कभी दोस्ती और आदत में।
जगहें अपनी समझ, अपनी बातें, अपनी अच्छाई और बुराई सब को अपने ही शब्दों में समेटे रखती है। और उसका ये समेटना जगह को बढ़ोतरी के पाएदान पर चढ़ा देता है।
क्योकि यहां आने-जाने वालों की कमी को महसूस नहीं किया जाता जिसमे बाहर से आ रहे शब्द जो बाहर के ही रहते हैं और अंदर बोले जाने वाली बोली जो सिर्फ वहीं की हैं, उस जगह को एक अलग ही जगह बना देती है।
किसी को यहां आना अच्छा लगता है तो किसी ने अपने जीवन के 10-12 साल के कई घंटे यहां दिये हैं, कोई यहां चैम्पीयन है तो कोई सिखना चाहता है, कोई रोज़ की चाय का शौकिन है तो कोई ठियों पर खड़े होकर चाय पीने को ही मज़ेदारी मानता है। सब अपनी ही धुन में है पर ये धुन सिर्फ लड़कों तक ही सीमित है अब वो चाय के ठियें हो या दुकान, कैरम क़्लब हो या वीडियो गैम की दुकान या फिर जिम....
सब अपने-अपने तरोकों से जगह से जुड़ते हैं उसे अपनाते हैं, उठते-बैठते हैं, मज़े करते हैं, खेलते हैं या खड़े होते हैं सबको अपनी जगह, मिलने वाला माहौल और आदत या शौक़ से लगाव है जो कि उस जगह से जुड़ा है।
सैफू...
बनने- बनाने के बीच में...
कुछ जगहें जो अपनी और दूसरों की संतुष्टि को पूर्ण करने की इच्छा ज़ाहिर करती रहती हैं। कुछ अनमोल ठिकाने जो बहुमूल्य कामों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। उसी में बैठे लोग अपनी खांचेदार ज़िन्दगी को जोड़ते जाते हैं, अपनी जरुरतों, कामों और महफिलों को जमाने में इच्छुक लोग घूमते, बनाते चलते हैं अपनी मनचाही जगाहों को।
यह लोग वो होते हैं जो छाल नुमा ज़िन्दगी को जीते जाते हैं और हर वाद-अपवाद को अपने शरीर से दूर कर नई छाल की बुनाई में लग जाते हैं।
फिर शुरु होती है समुह गढ़ने की एक अनुठी प्रतिक्रिया। जिसमें अवज्ञा और अनादर को दूर हटाकर अपने बनाए कस्बों मे विलीन होने की शक्ति होती हैं। वो कस्बें जो अन्नत में खत्म होते और फिर अपने प्रतिबिन्द की तरह ही बनते जाते हैं।
इसमे प्रकाश और अंधकार दोनों ही इन कस्बों को बनाने और बिगाड़ने में निपुर्ण है।
प्रकाश जो कि महफिल की रोनक में सब दिखाता है, सच हो या झूट। पर अंधकार अपनी चपेट में सब को लेकर विलीन होने की कंगार पर नज़र आता हैं।
इसमे सर्वदा अपना पाठ लिए घूम रहा हैं, जो टाईम-टेबल के हिसाब से आपको अपनी रुटीन में घूमाता रहता है। वो नवीन इच्छाओं को गाठ-व-गाठ बांधकर एक जालीदार ढ़ांचा तैयार करता है।
उसे आप ओढ़ कुछ हदतक लोगों की छायादार वाणी से बच पाते हो। मगर आप अंजान नहीं हो, क्योंकि जालीदार ढ़ांचे की वजह से आप अपने कुल में हो रहे संवाद को परखते और जोड़ते चलते हो...
...मनोज...
Labels: महफिलों के बीच से... , संवाद
" भाई ताब का कैरम क्लब "
पुरानी दिल्ली की रंग वाली गली में।
यहां लोगों के आने के कई तरीके है मतलब सबके अपने-अपने मतलब जुड़े हैं इस जगह से। यहां कोई खेलने आता है तो कोई देखने, कोई मज़ाक करने तो कोई खेल की भावना में मगन चैलेन्ज देता हुआ पर जब यहां की भीड़ अपने रंग में होती है तो पुराने खिलाड़ियों की वही मण्डलियां जो ऊच-नीच को शर्तो के बल पर तय करतीं हैं। जो कहती हैं
"है दम तो जीत के दिखा पर शर्त लगा कर" उस वक्त खेल पर खिलाड़ियों का पैसा भी लगा होता है और इज्ज़त भी, इज्ज़त तो दूसरी निकली आवाज़ से वापस भी आ सकती है पर यहां पैसों का जेब बदलना चलता रहता है। जिसमें लगता है कि यहां हर कोई अपना रुतबा तय करने की होड़ में है, ऐसे में ये देखते चहरे कि "कौन जीतेगा" बड़े उत्साहित रहते हैं कि किसने, कब, क्या गलती की और वो अगली टन आने पर क्या कर सकता है, ये वहां खड़े बाकी लोग अनुमान लगाते और कुछ-कुछ बोलते नज़र आते।
यहां शर्तों के दाम 200 से 500 तक का सफर तय कर लेते हैं सिर्फ अपने अनुभव की बहस पर। बिना बहस तो कोई यहां 100-50 की भी शर्त नही लगाता।
पर बिना शर्तों में हार-जीत का मज़ा लेते कई लोग जगह में खेल देखने और खेलने का आकर्षण बन जाते हैं शुरुआती या कभी-कबार दिखते चहरों के लिए।
...सैफू...
Labels: देखा-देखी , महफिलों के बीच से...
" रहीस रॉकेट "
हर किसी माहौल में मिलावटी दुनिया की कल्पना करना और अपने आपसी सुझावों को सुलझाने की एक क्रिया जिसकी मौजूदगी हर बार, बार-बार महसूस होती है इस जगह में। हर कोई लड़ता, भागता, सिमटता नज़र आता है। अंकुरों की फुटकान के साथ जन्म लेते हैं निर्णय जिसे पनपने की एक जगह के रूप में संजोए रखने की कोशिश करती है यह जगह। कितनी जगहों के नेटवर्क को अपनी आपसी बातों में छोड़ जाते लोग, कुछ पाते कुछ खोते लोग, कभी समाचार केंद्र बन कर उभरते, कभी बातों-बातों में मदरसे की तालीम देते, कभी आपके और समाज के बनाए नियमों से लड़ते तो कभी सब आँखें मींच कर छोड़ देते समय पर और इन्तज़ार करते समय कटने का।
क़्लब, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई लोगों के आगमन से सिमट सी गई है। दो बड़े कैरम से संजोया हुआ यह क़्लब 20 लोगों को अपने भीतर समेटने की क्षमता के साथ वहाँ अपना मुकाम जमाए खड़ा है।
रहीस नाम से जाना जाने वाला शख़्स चैम्प के ओहदे को समेट वहाँ अपनी मौज़ूदगी को रोज़मर्रा में बरकरार रख किसी के सामने खेलने बैठा है। जब उसका स्ट्राइकर गोटी से टकराता है तो गोटी रॉकेट की तरह अपना रास्ता बनाते हुए पॉकेट में चली जाती है। इसीलिए उसे रहीस रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है।
हर मुलाक़ात में मेहमान और मेज़बान की भूमिका को निभाने की रीत छोड़ कर रहीस भाई अपने दोस्तों की मण्डली को महकाने और चमकाने का सारा बंदोबस्त अपनी दमदार आवाज़ के साथ तैयार कर इन रिश्तों की गाँठों को खोलते नज़र आते हैं। बड़ी आँखों के साथ खिलाड़ियों के जज़्बातों के साथ खेलने के अनुभव के कारण कभी तो हार जाते हैं तो कभी जीत कर बातों की लड़ियों को इकठ्ठा करके हारने वाले को जला-जला के भून डालते हैं।
ऐसी ही बातें जो बकवास या छोड़ू हैं वे इन्हें यहाँ का बकवासबाज़ी का बादशाह बनाए रखती हैं। इनका ज़ोरदार सलाम करने का अंदाज़ पूरे क़्लब का माहौल बदल देता है। ये अक्सर कुछ ऐसी बातें कहते रहते हैं जिसका किसी को पाता नहीं होता। इनका कहना है कि ये 17 साल की उम्र में दिल्ली चैम्प का ख़िताब हासिल कर चुके हैं, लेकिन इनकी छवि को देखकर तो नहीं लगता कि इन्होंने कभी चैम्प के ओहदे को स्वीकारा है पर खेल और खेल में निशानेबाज़ी इनको वहाँ का चैम्प बनाए रखती है। इनकी अदाएँ लोगों को सर फोड़ने और विवश होने पर मज़बूर कर देती हैं। लोगों का इनकी बातों को सुन हँस-हँसकर पेट में दर्द हो जाता है।
इस हल्ला-गुल्ला वाले माहौल में एक समय ऐसा भी आता है जिसमें सबकुछ शांत हो जाता है। वो मग़रिब की अज़ान का वक़्त होता है जिसमें सभी लोग चुप हो जाते हैं। गेम खेलना और पंखा बन्द कर दिया जाता है। वहाँ बैठे चहरे एक-दूसरे के चहरे के चुप होने के इंतज़ार में लगे दिखाई देते हैं।
...मनोज...
Labels: महफिलों के बीच से... , संवाद
नज़रों से...
वो हमारी कालोनी में ही मंदिर के पास बने एक छोटे से कमरे में रहता है। उसका वो छोटा सा कमरा किसी इलेक्ट्रॉनिक कबाड़खाने से कम नहीं। उसने अपने कमरे में अपना एक कोना बना रखा है। चारदीवारी के बीच हर एक कोने में फैले पुराने रेडियो, घड़ियाँ, घंटे, अलार्म, कैमरे, पुराने वायर - कुछ ठीक तो कुछ ख़राब, जगह-जगह फैले खुले रेडियो के पुर्ज़े और उसके काम को अंजाम देने वाला हर वो सामान खुला पड़ा था, बिना किसी बॉक्स के।
उसकी इस चारदीवारी में कोई आलमारी नहीं है, बस एक टेबल है जो कोने में न होकर भी कोने में है। उस पर रखा था एक14 इंची टी.वी., जिसकी बंद मौजूदगी से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि "क्या ये टी.वी. ठीक होगा?" पर बात तो उस शख़्स की है जो 5फुट4-5 इंच का होगा। आँखों में हमेशा मेहनती नमी और कपड़े ज़्यादातर डार्क कलर के, चेहरा गोल और हाथों में ग्रीस जैसा कालापन - जो ये एहसास दिलाता है कि बन्दा मेहनती है।
वही कमरा उसके रहने की जगह है और वही खाने-पकाने की भी। वही उसका कारखाना है और वही चारदीवारी उसका माल इकठ्ठा करने का गोदाम।
वो हमेशा अपने कमरे में अकेला या दुकेला बैठा नज़र आता, कुछ न कुछ करता हुआ।
उसकी उम्र तो मुझे मालूम नहीं पर होगी यही कोई 30 के आस-पास की। वो अकेला ही रहता है। पता नहीं उसके माँ-बाप इस दुनिया में हैं भी या नहीं। आज तक मैंने उसे सिर्फ़ काम करते ही देखा है। कभी-कभार खाली दिखता है तो इतना खुश दिखता है मानो उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। कभी उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि "भाई क्या हालचाल है?"
अक्सर वो बाहर नहीं दिखता। हाँ, कभी-कभी चाय पीने ज़रूर निकलता है। ऐसे में उससे मुलाक़ात होना मुश्किल सा था। पर कुछ वक़्त पहले उससे हुई एक मुलाक़ात ने मेरे कई सवालों की गुत्थी सुलझा दी, मसलन वो कितने समय से इस काम में अपने पैर जमाए हुए है? कबाड़ चुनने-खरीदने की नज़र उसने कितने समय में बनाई होगी? पुराना आलार्म कितने में खरीदता-बेचता होगा?
उसके कबाड़ को देखकर इस तरह के ढेरों सवाल मन में उठते थे पर एक सवाल का जवाब वो हर सण्डे कालोनी को देकर निकलता है कि उस कबाड़ का वो करता क्या है? दीवार घड़ियाँ, नये-पुराने रेडियो, ठीक चलती हुई हाथ घड़ियाँ, यहां तक कि वो कभी-कभी टी.वी. भी लेकर निकलता है। वो इतना सामान कबाड़ से कैसे ठीक कर लेता है?
सच में उसकी मेहनत या कहें उसके दिमाग का खेल है। वो जैसे ही एक बोरे में सारा सामान कंधे पर लादे कई गलियों से गुज़रता है, रास्ते में मिलने वाला शख़्स पूछने से नहीं चूकता-"आज कोई बढ़िया अलार्म है?”, “कोई अच्छी सी घड़ी है?”, "यार बोरा उतार, शायद कोई बढ़िया रेडियो मिल जाये?”
ऐसी लाइनों से होकर गुज़रता वो कई बार बोरे को कंधे से ऊपर -नीचे, उतारता-चढ़ाता, बाहर तक पहुँचता और किसी रिक्शे की ताक में खड़ा हो जाता।
जैसे ही कोई रिक्शा रुकता तो वो बोलता, "भाई चलना है इतवार बाज़ार"
...सैफ़ू...
Labels: देखा-देखी , महफिलों के बीच से...
माहौल और समाज
माहौल और समाज हमे हमेशा एक धुंध में रखता है जिसकी वजह से हम कभी कुछ नहीं देख पाते इसी में समय अपने आप को बदल इतिहास लिखता चला आ रहा है। वो इतिहास जो अभी के समय हमारे साथ है और बाद में किसी कागज़ के पन्ने का एक हिस्सा सा लगता है।
उसी मे बंधे लोग बाद या आने वाले इतिहास की रचना किये बिना ही फैसले लेने और समझने की एक अनमोल गाथा को लोगों को समझाते आ रहे हैं।
अपने अनुभव और अपनी समझ में बनाए एक आकार को लोगों के आगे पेश करके वो रचनात्मक तरीके से जी रहे हैं।
वो पेश करना आगे चल समाज की आवाज़ या समाज का ही एक रुप ले लोगों को अपनी बोलियों में इनकी परिभाषाएँ देता चला आ रहा है।
चाय की दुकान जिसकी हालत से मालूम होता है कि वो काफी पुरानी है पर उस पुरानेपन को सफेदी की चमक से अभी भी चम्का रखा है।
चाय की दुकान जिसमें चाय बनाने का एक बड़ा सा ठिया, जिस पर तीन बड़ी केतलियाँ जिसमें हमेशा चाय पत्ती का पानी उबलता रहता, कप और गिलास की एक लम्बी लाईन तकरीबन पन्द्रह जोड़े और बीच में एक नीली मटमेली शर्ट पहने एक ढ़ाड़ी वाला आदमी जो हमेशा ऑडर की चाय बनाकर देता।
उसी के बराबर में एक सफेद कुर्ता-पजामा पहने, सर पर टोपी लागाए हाथ में अखबार लिए कुर्सी पर बैठा आदमी जो सबके पैसे काटता है।
दो लोग और जो चाय को सर्व करने का काम करते हैं। जो तकरीबन एक बारह साल का लड़का और एक पच्चीस साल का आदमी है।
यहां लकड़ी की छ: टेबल है और बारह बेंच। हर एक टेबल पर 4 लोग आ जाते हैं। एक कोका-कोला की फ्रिज़ जो अब वक्त़ के हालात के साथ अपना रहन-सहन बदल चुकी है, जिसमें अब कप-गिलास के सेट वगैरह ही रखे जाते हैं।
उसी के बराबर में दूसरी टेबल पर बैठी एक औरत जो उस चाय की पुरानी दुकान में नई सी लग रही है। उसने नीला लाईट सुट पहन रखा है, रंग सांवला, चेहरा थोड़ा लम्बा, काली और छोटी आँखें, होटों पर सुर्ख गुलाबी रंग की लिप्सटिक, दांत गुटके खाकर पीले कर चुकी वो औरत आज समाज की नज़रों से लड़ रही है।
कोई उससे कुछ कहता नहीं पर हर कोई उसे आँखों-आँखों में नग़्न कर बैठा है।
और वो सब बातों से अन्जान न होते हुए भी अपनी चाय में मस्त है।
...मनोज...
Labels: महफिलों के बीच से... , संवाद
इन्तज़ार में नहीं रहती जगह
किसी के इन्तज़ार में नहीं रहती जगह...
एक के जुड़ने के इन्तज़ार में नहीं रहती।
अपने आगाज़ के जमने का।
एक दुसरे से मिलकर अपने होने का एहसास दिलाने का।
कभी खेल के रूप में तो कभी अपने अंदाज़ में
जगह को पहचान देने का।
किसी के इन्तज़ार में नहीं रहती जगह...
पर उसमे रहने वाले उसे अपना-अपना कहकर
पुकारनें वाले जरूर इन्तज़ार में रहते हैं,
अपने होने के बहाव को दूर तक फैलाने के लिए,
अपनी चाहत से बनने वाली उस जगह को
किसी की चाहत का हिस्सा बनाने के लिए।
किसी के इन्तज़ार में नहीं रहती जगह...
रहते है वो लोग, जो इन्तज़ार में रहते हैं
अपने साथ जुड़ने वाले साथी को पार्टनर कहने को,
अपने आप में खोने में, समाज क्या होता है? क्या कहता है?
उसकी परिभाषा से दूर अपना उस जगह का
समाज तैयार करने में।
किसी के इन्तज़ार में नहीं रहती जगह...
इन्तज़ार में रहते हैं वो ठहाके जो कभी हां-हां में बाहर आते हैं
तो कभी दबी-दबी सी आवाज़ों में, इन्तज़ार में रहते है वो
जो कहते हैं कि आज का दिन अलग-अलग सा है
पर फिर भी रोज़ की तरह है।
आज रात नींद नहीं आई पर ये तो रोज़ का रोना है।
एक जगह चाहिए जहां वो अलग होकर भी अलग न लगे
और रोज़ का रोना होते हुए भी कुछ अलग हो उस रोने में।
किसी केइन्तज़ार में नहीं रहती जगह...
पर इन्तज़ार में रहते हैं वो जो इसको
अपनी आदत का हिस्सा बना चुके हैं।
इन्तज़ार में रहते हैं उसके शुरू होने के,
पर इन्तज़ार में नही रहती जगह कि मैं कब खुलूंगी?
कब मुझे शुरू किया जाएगा?
इसको शुरू करने वाले इंतेज़ार में रहते हैं कि
अपना भी कोई ठिकाना हो जहां
चार बातें अपनी हों और चार बातें सामने वाले की भी
जिसमें सिर्फ़ बातें ही ना हों,
हो वो जो बातें भी हों और कोई इशारा भी कि
हां है कोई इन्तज़ार जिसके इन्तज़ार में
इस जगह के बनने की शुरूआत हुई।
सैफूद्दीन
Labels: संवाद
जगह का मालिक
::: भाई आलू के नाम से जाना जाता है पता नही यह उनका नाम है या उनके मोटे शरीर के कारण रख दिया गया है। वो हमेशा नहा-धोकर, सफेद रंग के कपड़ों में अपने कैरम क्लब की नियमित रोज़मर्रा में आने वाले लोगों का स्वागत् करते रहते हैं। उनका यह मेज़बान का काम इस घूमती-फिरती पुरानी दिल्ली में दोपहर के 4 बज़े से रात के 1 बज़े तक चलता है।
जिसके बीच उनका खाना-पीना और सोना सभी उस जगह में होता। इस बीच लोग आते, खेलते और महफिलें जमाते जिसमें भाई आलू भी शरिक होते।
पर भाई आलू को कैरम खेलना नही आता उनका तो शौक़ पंतग उड़ाने का है और उनका वो शौक हमे कैरम क़्लब की दिवारों पर दिखाता है। उन्होने अपने क़्लब की क्रिम सफेदी के ऊपर कई तरह की पतंगें लगा रखी हैं जो उनके बीते समय को कहीं रोकी सी लगती हैं।
उन्हें अपना कैरम क़्लब साफ रखना पसन्द है, पर वो उन्हे भी मना नहीं करते जो अपनी पान की पीकों से दिवारों को गन्दा करते हैं। उनके लिए उन्होने कुछ छोटी बाल्टीयां लगा दी हैं जिसमें वो थूकते और पिचकारियां मारते नज़र आते हैं।
इसी तरह के सारे इन्तेज़ाम भाई आलू ही करते है। जगह उनकी ज़्यादा बड़ी तो नहीं पर उन्होने अपने क़्लब में दो कैरम लगा रखें हैं जिसमें एक बार में आठ लोग खेल सकते हैं। किसी को परेशान किये बीना ही सब अपनी मर्जी का खेल, खेल सकते हैं, हसना, चीखना-चिल्लाना जैसी अव़ाज़ों से वहां की जैसे शान सी बड़ती हो पर अपनी अंदरूनी छवि को हमेशा बाहर से दूर रखती है ये जगह। अपने अन्दर जमी चीज़ों को पिघलनें से पहले ही खत्म कर देती है।
मनोज
Labels: देखा-देखी
कुछ जगहें...
चलते रास्तों पर अपना एक ठहराव लिए कुछ जगहें जो आपको रुकने-ठहरने का आमंत्रण देतीं हैं।
वो जगहें जो अच्छे-बुरे की परिभाषा को लिए आपको कुछ और समझाने की कोशिश में लगी दिखाई देतीं हैं।
कभी तो वो मंचन बन आपको ऊँचा उठा देतीं हैं तो कभी उस ऊँचाई से धक़्का भी दे सकती हैं।
जगहें जो अपने निरंतर बदलाव के साथ अपनी बदलती परिभाषाओं में आपको समेटती रहतीं हैं।
उस समेटने मे आप उस जगह के एक बदलाव मे गठित नज़र आने लगते हो।
वो गठन जो आपको एक लम्बे समय से अपकी बोलियों में आपको डराता नज़र आता था।
जगहें जो खालीपन और भराव दोनों में ही अपनी एक रोज़र्मरा को लिए जीती चली जाती हैं।
वो कभी सीखने का केन्द्र बन उभरती हैं तो कभी रिश्तों की डोर मज़बूत करती नज़र आती...
अपने बनने और दूसरों के बनने तक यह हमेशा लोगों को सींचती नज़र आती है। लोगों को रियाज़ मे
रखकर यह उनकी एक अलग छवि लोगों के सामने पेश करती हैं।
लोग उस छवि को कुछ और समझ अपने रियाज़ को पक़्का करते रहते हैं। अपनी समझ में जगहों के बीच होने वाले आदान-प्रदान की भावना को भूल वो आपसी समझ की दिवारों में घिरे रह जाते हैं। और बनाते फिरते है ऐसे माहौल जो कभी अच्छे लगते हैं तो कभी उसे बनाने वालों के लिए अच्छा और देखने वालो को लिए कुछ और ही ।
मनोज
Labels: महफिलों के बीच से...
"बचपन शायद अब भी है मेरे पास”
मेरी छोटी पैंट की जैब, जिसमें मुझे आज एक सिक्क़ा मिला थोड़ा ज़ग खाया हुआ और बहुत पुराना, ये उस जैब से मिला जिसमें पैसे कम और वीडियो गैम के सिक्क़े ज्यादा हुआ करते थे। एक जैब में सिक्क़े और एक जैब में चीज़ (टोफियाँ,चूरन) हुआ करती थी और शर्ट की जैब हमेशा खाली, पता नही क्यूं मैं उस जैब में कुछ नहीं रखता था?
ये सवाल तो कभी मैंने अपने बचपन से भी नहीं किया और न ही उसकी कोई जरूरत थी।
मुझे तो बस अपनी पैंट की उन दो जैबों से मतलब था जो कभी खाली नही रहती थी क्योंकि उस वक्त मेरी अम्मी की दी हुई वो अठ्ठन्नी ही काफी हुआ करती थी मेरी जैबें भरने के लिए और बाक़ी में अपने अब्बू से मांग लिया करता था। इस तरह मुँह बनाकर कि जैसे मुझे आज किसी ने पैसे ही नहीं दिये, तब मुझे मेरे अब्बू भी एक रूपया या अठ्ठन्नी दे देते थे और उस एक या ढ़ेढ रूपय में मैं अपनी दिनचर्या बड़ी खुशी-खुशी गुज़ारता था।
मुझे याद हैं वो दिन जब मैं वीडियों गैम की मार्किट में सुबह से शाम कर दिया करता था
सन् 1990-92 के वो दिन और शामें मुझे बखुबी याद रहते हैं, जब मैं स्कूल का एक रूपया भी संभाल कर रख लिया करता था और घर आते ही मेरा सारा ध्यान वहीं लग जाता था कि मैं कब और कैसे घर से निकल कर वीडियो गैम की दुकान में पहुच जाऊ।
बाहर आते ही मैं अपनी जैब टोफियों और चूरन से भर लेता और बचा के रखता " अठ्ठन्नी "
जिसमे तीन सिक्क़े मिलते थे। वीडियो गैम की दुकान का आधे से ज्यादा अंश मलवे के ढ़ेर में रहता था और खाली की गई जगह में 10-12 वीडियो गैम की मशीनें लगी रहती थी।
मलवे के लिए कोई छत नहीं थी पर उस दुकानदार ने उन मशीनों के लिए छत बनवा रखी थी पर उसमें एंटर होने के लिए कोई गैट नहीं था।
तीन दिवारी के आगे तीरपाल का परदा लगा रहता था। मानो कोई दुल्हन घूंघट में अपने चहरे को छिपाए बैठी हो।
मैं उस दुकान मे जाते ही बहुत ही खुश होता था जैसे वहां का माहौल ही मेरी जिंदगी का मोल हिस्सा हो। सिक्क़े लेकर मैं किसी ऐसे गैम की तलाश में खड़ा हो जाता जो खाली हो, जिसमें मैं अकेला खेल सकू। वहां हमेशा भीड़ रहती थी खासकर तब जब मैं जाता था दोपहर से शाम के बीच, स्कूल की छुट्टी के बाद। घंटो-घंटो वीडोयो गैम की शक्लों को तकता और जब खाली मिलता तो खेलने का लुत्फ उठाता, मुझे हमेशा अकेले खेलना मतलब वीडियों गैम से चैलेंज़ करने में बड़ा मज़ा आता था पर ज्यादातर मुझे कोई अकेला खेलने नही देता था क्योंकि वहां भीड़ ही इतनी रहती थी कि जिसमें मौका मिले खेललो।
वहां भटकते चहरे हमेशा एक लालसा में मिलते थे कि कोई मिले जिसे हरा सकू या उससे मज़े ले सकू अपने गैम के बल से चहरों के भाव एसे बदलते थे जैसे मिनट से पहले सेकंड की सूई का 60 बार बदलना। मेरे साथ जो भी खेलता हमेशा मेरा गैम ऑवर करके हंसता और कभी कोई गाली बक़ देता तो कोई सर पर हाथ फ़ैर घर जाने को कहता।
कभी भी चैलेंज में जीत नही पाता था मैं और न ही उस वक्त मैं किसी को मना कर पाता था कि मेरे साथ मत खेलो मुझे अकेले खेलनें दो...
कोई मुझसे बड़ा होता था तो कोई हमउम्र सबको खेलनें से मतलब था न कि मुझसे कि मुझे ढ़ग से खेलन आता है या नहीं, बस गैम ऑवर कर दिया करते थे और मैं फिर से किसी मशीन के खाली होने के इंतेज़ार मे लग जाता...
इसलिए मैं ज़्यादातर अपना टाइम दुसरों का गैम एंजोए करने मे ही गुज़ारता था क्योंकि मुझे डर रहता था कि मेरा गैम ऑवर हो जाएगा तो मैं और सिक्क़े कहां से लाउंगा, हमेशा सिक्क़े बचा कर रखता था। इस तरह वक्त गुज़ारना कभी-कभी मुझे नुकसान देता था।
जिसको मैं अपनी गलती नहीं मानता था, जिसकी वज़ह से मुझे घर पर डाट तो कभी-कभी मार भी पड़ती थी।
पर हंसने वाली बात तो ये है कि मैं बाज़ नहीं आता था और वहां रोज़ जाता था डर को डर की शक्ल में छोड़ मैं अपने मज़े को अपनाने उस वीडियो गैम की दुकान पहुँच जाता था।
वो दिन बड़े हसीन पल हुआ करते थे जब मैं अपनी ज़िम्मेदारीयोंऔर रोज़ के खर्चे की समझ से दूर मज़े किया करता था। आज जब मैं उस दुकान में गया और उस दुकानदार से मिला जिसका मैं अब नाम तक नहीं जानता तो उन यादों को ताज़ा करने का मन कर बैठा।
खैर अब भी वो दुकानदार अपनी दुकान को वैसे ही चला रहा है पर अब मेरे बचपन और दुकानदार के साथ-साथ उस जगह की भी शक्ल बदल चुकी है। अब वहां वो मलवा नहीं है, न ही वो तीन दिवारी बची है और न अब यहां सिर्फ़ 10 मशीने हैं। अब ये वो मार्किट नहीं जिसमे मेरा बचपन खेला करता था, आज ये बहुत बड़ी दुकान बन चुकी है। दुकान के ऊपर तीन मंज़ीला बिल्डिंग खड़ी हो गई है, दुकान मे 20 से 25 वीडियो गैम की मशीनें हैं और अब यहां वो अकंल जो पहले दुकानदार हुआ करते थे वो सिर्फ़ बैठे रहते हैं। इतनी भीड़ को संभालने के लिए अब यहां एक काउंटर बना हुआ है जिसमें उनकालड़का बैठता है और पैसे लेकर सिक्क़े देता है।
अब यहां अठ्ठन्नी नहीं चलती पर सिक्क़ा अठ्ठन्नी का ही है एक रुपय के दो सिक्क़े।
पर मेरे पास अब भी वो एक सिक्क़ा है जो मैंने अठ्ठन्नी के तीन में लिया था...
सैफूद्दीन
Labels: यादों की दुनियां...