हमेशा से जगह अपने अंदर कई बातें, कई किस्से छुपाए बैठी होती है। अलग ज़ुबान और अलग अलग किस्से-कहानियाँ बदलती पीढ़ी में भी बातों और यादों के ज़रिये अपना सफर बरकरार रखती हैं। लोगों का दोहराना और बातों-बातों में बातों का फिसल जाना चलता रहता है जिससे कई महफिलें और मजमे अपने आपको रोज़ना की दौड़ में जमा पाते हैं। एसे ही बातों-बातों में पुरानी दिल्ली के भी कई किस्से तरह-तरह की ज़ुबानों और उम्र के साथ सामने आए कुछ सुनने में इतने रोमांचक लगते कि मानों बस सुनते ही जाओ तो कुछ उम्र दराज़ आवाज़ में दम-खम के साथ पेश आते हैं।
जामा मस्जिद चौक का ख़म्बा...
हम उसे पुराने दोर का खम्बा भी बोल सकते है।
कई साल पहले जामा मस्जिद चौक पर एक बड़ा सा ख़म्बा हुआ करता था जो इस समय हमारे साथ नही रहा। सुनने में आया है कि उसे सड़क बनाते वक़्त हटा दिया गया था क्योंकि वो सड़क को चौड़ा करने के काम मे आड़े आ रहा था। हमारा मानना था कि उस ख़म्बे के बारे में कोई बुजुर्ग ही हमें अच्छा किस्सा सुना सकते हैं क्योंकि समय के साथ जी चुके लोग समय को उसी रंग में दिखाते हैं जो उसका रंग था। लेकिन जब कई रंग की कहानियों से किसी पन्ने को रचा जाता है तो उसे हम रंगीन कहते है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और उसी रंगीन पन्ने की तलाश में हम पहुचे चितली क़बर चौक जहां रोज़ रात कुछ बुजुर्ग बाज़ार की दुकान बन्द होने के बाद उसके तख़्त पर अपनी पुरानी यारी-दोस्ती के किस्सों से, कुछ आज से कुछ कल से वहां महफिल सजाते है। मिलने की सोच थी कि अगर हम उनसे ख़म्बे के साथ जुड़े लम्हों के बारे में पूछें तो कई तरह की कहानियाँ- यादें और घटनाए सामने आएंगी।
ये सब बुजुर्ग आस-पास से इकठ्ठा होकर इस जगह में मिलते है सब एक-दो साल कि छोट-बड़ाई से एक-दूसरे के साथ रहते आए है जिनमें से कुछ जान-पहचान के हैं तो कुछ अंजान लोग, आते-जाते इनसे दुआ-सलाम का सिलसिला तो सालों से चला आ रहा है पर कुछ नए सिलसिलों की शुरूआत इस बार हुई है।
लगभग सभी सफेद कुर्ते-पेजामें की पोशाक में है जिसमें टोपी भी शामिल है। इनका आपसी तालमेल बहुत ही शांत तरीके से माहौल में दिखाई देता है जिसमे से शौर और हा-हा-ही-ही कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता, पास जाने पर सबके चहरों पर खिलखिलाहट जरूर दिखती है। इनके बीच शामिल होने के लिए न जाने क्यों किसी तैयारी की कमी महसूस हो रही थी पास जाने पर समझ आ गया था कि तैयारी बस अपने रवइयें की करनी थी। क्योंकि जब कोई न-पसंद हो जाता है तो उसका उनके बीच में रहना न-मुमकिन हो जाता है।
हम – अस्सलामु अलेयकुम.....
( सलाम ही महफिल में आपको इज़्ज़त देता है, आपके सलाम के जवाब के साथ )
वालेयकुम अस्सलाम- सबकी आवाज़ में जवाब हल्की सी गूज़ बनकर सुनाई दिया।
दुआ-सलाम के बाद हमने उनसे कुछ पूछने की इजाज़त मांगी तो जवाब "पूछो-पूछो" में मिला।
मैं – आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, ( किसी एक चहरे की तहफ देखते हुए )
अब्बा जामा मस्जिद चौक पर पहले एक ख़म्बा हुआ करता था उसके बारे में जानना था कि वो कब से कब तक था और लोग उसके साथ कैसे जिया करते थे?
"हम उनकी सुनाई हर एक बात को बड़े ही एहतियात से सुन रहे थे"
अब्बा - हां था। और वो अब का थोड़ी न था, हम खुद उसे अपने बचपन से देखते आए थे।
मैं - कैसा दिखता था वो ख़म्बा ?
अब्बा - अरे वो बहुत काला था चौड़ा और लम्बा भी था उसके निचे गोल चबूतरा बना हुआ था जिस पर हम भी जाकर बैठ लिया करते थे।
अब्बा काफी बुजुर्ग थे इसलिए उन्हें अब्बा कहना अच्छा लग रहा था और उनकी बातों से लग भी रहा था कि वो बहुत कुछ बता सकते है, अब्बा की आवाज़ में ज़रा सी भी झिझक नहीं थी किसी भी बात को बताने में।
मैं - हां हम उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि लोग उस खम्बे को अपनी ज़िंदगी में कैसे जिया करते थे?
अब्बा सबकी तरफ देखते हुए बोले- सबकी तो नहीं पता पर हां उसका अपना बस एक ही किस्सा है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है जितने भी हम बैठे हैं तुम्हें छोड़कर।
यहां के किसी भी बुजुर्ग से पूछ लेना कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो बारात कहां से घूमाकर लाए थे... किसी पुराने आदमी से ही पूछना जो जामा मस्जिद इलाके का हो हमारी तरह।
"अब्बा का खुद के साथ, साथ बैठे सभी को पुराना कहने पर सब हसने लगे... एक-दूसरे की तरफ हँसी की दावत देते चहरे हमें भी हँसी के कुछ पल दे गए अपने बीच।"
मैं - बारात घुमा कर लाने का क्या रिवाज़ था ?
अब्बा - कोई रिवाज़ नहीं था, बस यूहीं...
मैं - यूहीं मतलब ?
अब्बा - हम कितनों की ही शादियों में नाचे, कुछ अपने, कुछ अंजान पर सबकी एक दिशा हुआ करती थी बाज़ार से होकर जामा मस्जिद के ख़म्बे तक फिर ख़म्बा घूमकर बाज़ार से होते हुए वापस घर। सबके साथ इतना सोचा नहीं था कि ये क्या रिवाज़ है? पर जब खुद की शादी पर बराती खम्बे की ओर चलने लगे तो चलने से पहले मैंने अपनी अम्मी से पूछा- अम्मी ख़म्बे तक क्यू जा रहें है हम? हमे तो बस पास मैं ही जाना है, कोई रिवाज़ है क्या ? तो अम्मी ने कहा- अरे बस यूहीं।
जब से मैं भी इतना ही जानता हूँ कि वहां शादियों पर लोग चक्कर बस यूहीं लगाया करते थे।
बराबर में बैठे बुजुर्ग ने भी इसमें अपनी बात जोड़नी चाही।
अंकल - चक्कर लगाना कोई जरूरी नहीं था मर्ज़ी वाली बात थी पर अगर कोई खम्बे का चक्कर नहीं लगाकर आता था तो बरातियों में से कोई न कोई पूछ ही लिया करता था- ख़म्बे का चक्कर क्यू नहीं लगाया?
कुछ बेफज़ूल की बात बता कर इस सवाल को टाल दिया करते थे तो कुछ सोचते थे लगाने में कोई हर्ज नहीं था लेकिन बात कुछ और थी। हमें तो लगता था कि जैसे ये कोई बादशाही वक़्त की रीत की तरह चल रहा था।
मैं - वैसे वो खम्बा वहां कब से था ?
अब्बा और कइ ज़ुबानों ने आगे-पीछे बोलते हुए जवाब दिया- हम सभी अपने बचपन से उसे देखते आए है और शायद वो पुराने वक़्त से ही है।
अब्बा - पहले उसके पास से होकर ट्रैन गुज़रा करती थी, चावड़ी, सदर, नई सड़क, यहां और लाल किले जैसी कई जगह से होकर वो पुरानी दिल्ली में घुमा करती थी वो जामा मस्जिद के इस ख़म्बे पर भी आकर रुकती थी पर वो अपना एक वक़्त हुआ करता था मोज-मस्ती का, घूमने-फिरने का।
अच्छा तो अब हम इजाज़त चाहते है अभी के लिए पर हम आते रहेंगे और हां अब्बा ये ट्रैन वाली बात continue रखेंगे।
ये कहते ही सब हसने लगे और माहौल में हा-हा-ही-ही की आवाज़ आज पहली बार सुनाई दी।
सैफू.
कोई रिवाज़ नहीं था, बस यूहीं...
Monday, September 07, 2009
Labels: महफिलों के बीच से... , संवाद

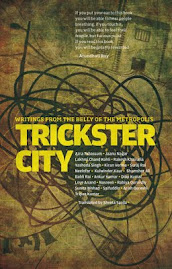
2 comments:
hue mehnge bahut chiraag
chota chitta likha karo.
बहुत बढ़िया लिखा है आपने! मुझे बेहद पसंद आया! आपकी लेखनी को सलाम!
मेरे नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है-
http://ek-jhalak-urmi-ki-kavitayen.blogspot.com
Post a Comment