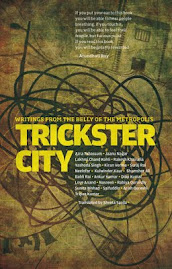चहरा लटकाए मैं अपने आपको कोस रहा था। इधर-उधर देखा कोई नहीं दिखा तो अपने आपको ही देख लिया। काश कोई दिख जाता तो सकून तो होता कि इस तन्हा रात में मैं अकेला नहीं हूँ।
पर मैं अकेला ही था, न अपने आपसे बातें करने का मन था और ना ही किसी ओर से पर फिर भी किसी को देखने की आस थी जो मुझे इस अकेलेपन से बाहर खींच सके।
लेकिन मैं अपने आपको क्यू कोस रहा था ? सिर्फ़ इस वजह से कि मेरा रास्ता अभी और भी है, और मैं चल रहा हूँ। न भागता हूँ और न छलांग लगाता हूँ, कहीं टकराता हूँ तो गिर जाता हूँ एक बार नहीं कई बार और जिस चीज़ से मैं बार-बार टकराता हूँ तो उसे लांगता क्यू नहीं?
सवाल तो कई लाई है ये रात पर जवाब नही लाई, अपने कालेपन के साथ-साथ मेरे जवाबों पर भी काली परते चढ़ा रखी हैं इस रात ने।
बार-बार आस-पास का संनाटा मेरे कानों में आकर सिमट जाता और मैं फिर एक बार घबरा जाता ये सोचकर कि
" काश कोई और भी होता इस रात में। "
सैफू.
रास्ता अभी बाकी है।
Labels: संवाद
"लोगो की शिरकत"
पुरानी दिल्ली के कई कौने अपनी-अपनी खासियत से मशहूर हैं। और उनका मशहूर होना यूही नहीं बना वो बनना चला आ रहा है पीढ़ीयों से, लोगों की पसंद से वो पसंद जो जगह और लोगों के बीच के धागे मे गीठा लगाऐ हुऐ है।
जिसे खोलना या खींच कर तोड़ देना आसान नहीं है। सरकार ने ऐसी कई उम्मीदे लगाई हुई थी पुरानी दिल्ली को लेकर पर बड़े-बूड़ों का साथ और लोगों का जगह से एक खास रिश्ता हमेशा सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरता आया है।
जामा मस्जिद की मरम्मत से लेकर बाज़ारों की रोनकों तक सरकार ने हाथ फैरना चाहा जिसे कुछ चीज़े धुंधली हो जाऐ लेकिन लोगो का जगह से रोज़ का जुड़ना और माहौल के बनने से बनाने की परिक्रिया मे रेहना सरकसर को पुरानी दिल्ली को छूने तक नहीं देता ।
सरकार चाहती है कि बदलती दिल्ली में पुरानी दिल्ली का भी वजूद बदले, चल रही पीढ़ी को नए नियमों के साथ जीना आ जाऐ गलियां बदल जाऐं, लोगों का बरताव बदल जाऐ जिसमे पुरानी दिल्ली भी बदलती दिल्ली का ही हिस्सा लगे यहां भी लोगो के साथ बदलाव चले ।
लेकिन हम इस पीढ़ी मे भी वैसे ही जीते है जैसे हमारे बड़ो मे पुरानी दिल्ली को जिया है वो मज़ा जो उन्हें सुनने मे आता है उनके मज़े के आगे अपना मज़ा कहीं फीका सा लगता है और उसी मज़े को और मज़ेदार करने की कोशिश मे लोग और जगह दोनों जीये चले जा रहे हैं मस्ती में।
सैफू.
Labels: संवाद
चैलेंज
"भाई वसीम दो रुपय के सिक्के देना ।"
गैम की दुकान मे दखिल होने का यही तरीका था मेरा। यहां के वीड़ियो पार्लर में गैमों की भरमार है यहां तकरीबन 20 गैम की मशीने है जिसमें से 2 गैम एसे है जिसमें 999 तारीके के गैम खेल सकते है। पर मेरा मनपसन्द गैम एक ऐसा गैम है जिसमे दो लोग एक साथ चेलेंज कर सकते है और यही चेलेंज हमें जीतने और हारने जैसी प्रक्रिया मे रखता है ।
मुझ पर घर वालों का डंडा भी हैवी होने लगा था । रोज़ घर वालों की सुनता पर मानता अपने दिल की । रोज़-रोज़ दो-दो घंटो के लिये गायब रहता और जब घर वाले पुछते "कहा था ?"
तो बतोलेबाज़ी दे कर घुमा देता । पर डर लगता उनके होने के एहसास से जिसमे मे शामिल भी होने से कतराता था ।
एसी जगहें जिसमे कुछ करने की, कुछ सीखने की प्रक्रिया मे खोने के एहसास को लोग या समाज़ कुछ अलग बोली या नज़र से सम्बोधित करते है । पर वो समाज वो लोग दरासल में हमारे घर वाले ही होते है, जो इस समझ को बनाए बैठे हैं ।
: कि मेरा बच्चा सीखने जा भी रहा है तो गैम जिसका सीधा मतलब खेल होता है, किस के मां-बाप चाहते है कि उनका बच्चा पढ़ाई की उम्र में अपना ज्यादातर वक्त खेल मे लगाए...
लेकिन खेल ही तो है जो सबसे पहले घर वाले बच्चे को सिखाते है और बाद मे उसी से दूर भगाने की कोशिश...?
मेरा खुद से खेल को सीखना और मेरे घर वालों का किसी खेल को सीखाना दोनों किस संदर्भ मे अलग-अलग दिशाऐं देते हैं ?
सोच और गलत धारणा के साथ बच्चे कुछ सीखने के साथ-साथ कई अलग चीज़े भी सीख जाते है जिनकी उन्हे उम्मीद भी नही होती ।
पर मेरे साथ एसा नही था ! घर वाले कहते-कहते थक जाते मगर मैं बाज़ नही आता, उनके मना करने के बाद भी मैं गैम खेलने रोज़ पहुच जाता और उनके आने पर उस दुकान के किसी कौने मे छिप जाता... अब तो इतना हो गया था कि मेरे घर वाले जैसे ही आते तो गैम का मालिक( भाई वसीम )मुझे इशारे से पहले ही बता देते और कभी-कभी तो मम्मी को बाहर से ही मना कर देते कि "ऐबी तम्हारा बेटा यहां नही है ।"
अब मेरा घर से गैम और गैम से घर आना आसान हो गया था ।
जब कभी मम्मी पूछती : तू गैम मे से आया है ना ? तो मैं मना कर देता और साथ मे ये भी कहता
: भाई वसीम से पूछ लो जाकर अगर मैं झूट बोल रहा हूँ तो ?
वो मेरे ये बोलने से कभी भी वहां पुछने नही जाती थी ना जाने क्यू ?
वो मेरी बातों का यकिन था या कुछ और मुझे नही पता... पर उन्हे इतना तो मालूम था कि मै रोज़ गैम खेलने जाता हू ।
अब तो मम्मी ने भी मुझसे रोज़-रोज़ पुछना बन्द कर दिया था । पर कभी-कभी बाई-चांस पूछ लेती थी तो उनका पूछना और मेरा जा कर भी मना कर देना चालता रहता । मैं अपने गैम से खुश था इसलिए मै बतोलेबाज़ी का उस्ताद बन गया और घर वालो को घुमाता रहता अपनी बातों से ।
इस बीच मेरे गैम में काफी सुधार आ गया था और मेने गैम खेलने के काफी तरीकों को अपने ज़हन मे बिठा लिया था, मैं अपने बराबर या अपने हमउम्र लड़को का भी गैम ओवर कर दिया करता था , एक सिक्क़े मे रानी मिलाना और स्कोर बनाना मेरे दाए हाथ का खेल था। पर अब भी मैं भाई लईक से चेलेंज करने से डरता था, उनकी मोज़ूदगी में मैं अपने आप को कहीं छोटा सा महसुस करता था ।
उनके साथ ना खेलना मेरे लिए एक पहेली सा बन गया था जिसे समझ पाना मुशकिल सा लगता था। एक कोने मे खड़े होकर चुपचाप उनके गेम को देखता रहता था । यह देखना भी मुझे काफी कुछ सिखाता । इसी से मैं अनेक सीखने-सिखाने की छुआन को उस कोने मे खड़ा सीखता रहता ।
एक दिन भाई वसीम ने कह ही दिया कि : कब तक खड़ा रहेगा ? कभी तो खेलेगा ही ?
" चल सिक्का डाल ।" उन्होने यह कहकर मेरा सिक्का उस गैम मे डालवा दिया । मैं खुश नही था मुझे पता था कि मेरा सिक्का बेकार गया । यह अभी दो मिनट मे मेरा गेम ऑवर करके भागा देंगे मुझे। इनके सामने मेरा तो गेम ऑवर होना तो तय है । इन्ही को तो देख कर सिखा हु भाला केसे हरा पाऊंगा इन्है ? अब सिक्का डाल ही दिया है तो खेलना ही पड़ेगा ।
उस जगह थोड़ा चेलेंज स्वीकारा लिया मैंने और उनके साथ खेलने लगा ।
वो मेरे साथ मज़ाक से खेल रहे थे उनका उनका कहना था की मेरे तीन पिल्यरों को एक से ही मार देंगे । इसलिए वो मुझसे मज़ाक से खेल रहे थे । उनके मज़ाक के खेल से भी मैं जी-तोड़ मेहनत करके लड़ रहा था । पता नही मुझसे खेला क्यो नही जा रहा था। क्या ये सब उनका डर था या गैम ऑवर होने का ?
उनके दो पिल्यर मर गये थे और मेरा एक । उन्होने मेरा दूसरा पिल्यर भी बच्चे की तरह मार दिया । पर तीसरे पिल्यर से मैंने उनका पिल्यर मार दिया । मैं मन ही मन खुश था उस समय मैंने उनसे दूसरा सिक्का डालने को मना कर दिया ।
वो भी हसी मज़ाक करते हुऐ आपने घर चल दिये । मन ही मन मैं खुशी से भरा था की भाई लईक को घर चलता किया है मैंने। इस बात को मैं हफ्ते भर तक गाता रहा था भाई वसीम की दुकान में ।
मनोज.
Labels: महफिलों के बीच से...
"मीना बाज़ार"
पुरानी दिल्ली की छोटी-बड़ी मंडलियों को समेट कर अपनी पहचान को पक्का करती ये ठिऐ नुमा दुकान मीना बाज़ार की सीढ़ियों पर एक ऐसा माहौल तैयार करती है जिसमे एक को देख एक मस्ती मज़ाक, जोरा-जोरी, लड़ाई-झगड़े से माहौल को भारी-भरकम बनाऐ रखते है। जो देखने-सुनने, उठने-बेठने मे बड़ी ही मज़ेदार जगह लगती है,
पर ये मज़ेदारी का एहसास कहां से आता है?
क्या जिस माहौल मे हमारा उठना-बेठना नही होता वो मज़ेदार या अदभुत होता है?
या हम ही से बनी जगह का एहसास जगह को खास बना देता है?
लोगों की शिरकत और एक ऐसे टाईम में दुकान का चलना जिस टाईम में लोग ढूढ़ते है ऐसी जगहों को जिसमे बैठ रात कट जाऐ, जिसमे रात का अंधेरा मन को सकून दे।
अलग-अलग छवियों, माहौलों और बातचीत से बनाऐ रखती है ये जगह अपने आप को दूसरों से अलग।
सैफू.
Labels: महफिलों के बीच से...
छवि, जगह और सोच.
छवि...
जिसकी अपनी एक पहचान, नाम और अदा हो, जिसके होने और न होने से जगह और सोच को बोलने के तरीके मिलते हैं।
वो तरीके जो छवि की पहचान से जोड़ कर समाज में रखे जाते हैं कभी नसीहत तो कभी सीखने-सिखाने की बोलियों में...
छवि वो भारी शब्द है जो माहौल की रूपरेखा पर अपनी छाप छोड़ बयां करने और देखने के नज़रिये को बदलने की क्षमता रखता है जिसमें कभी आप बदले-बदले से लगते हो तो कभी आपकी शख्सियत और स्भाव....
जगह...
जो फैलते, सिकुड़ते आकार में नाप-तोल करके बोली या देखी जाती है, जिसके बया पर उसको किसी नाम से पुकारा जाता है... और वो बोले जाने वाले नाम जगह में अपने मतलब को तलाशते फिरते हैं किसी की आँखों मे, किसी की बातों में तो कभी वहां भटकते चहरों में कि आखिर ये बक़चौदियां क़्लब है कहां?
ये नाम किसी कैरम क़्लब को वहां के बड़बोलेपन की वज़ह से दिया गया है। जगह का मालिक इस जगह को नाम देता है फैंसी क़्लब पर वहां की रिज़मर्रा मे शरीक होने वालों का यहां कहना है कि किसी से भी पूछ लैना बक़चौदियां क़्लब कहां है? तो वो सीधा यही का पता देगा।
जगह और नज़रियें दोनों एक दूसरे से लड़ते नज़र आते हैं कभी देखा-देखी मे तो कभी कहा-सुनी में। जिसमें नज़रियां बदले या न बदले जगह बिना किसी बदलाव के नामों से बनी पहचान को बदलती रहती हैं।
सोच...
बोलने और संभलकर बोलने के बीच की समझ जो कि सोचकर बोलने की भाषा को तैयार करती है। और वही सोचकर बोलना ज़हन में जगह और छवियों को गाढ़ा करने के माद्दे को और गहरा कर देता है जिसमें हम कभी खोए-खोए से कहलाते हैं तो कभी अपने मे मगन से।
पर यही सोच शख्सियतों को जगह भी देती है तो कभी अपने में न होने का एहसास भी दिलाती है।...
"नंगा नहाएगा क्या और निचौड़ेगा क्या?"
ऐसे मुहावरे किसी सोच मे बहते है जिसमें हम अपनी बोली लाईनों में किस सोच को किसी की ओर फैंकते हैं उसको समझ या समझापाना कभी साफ तो कभी धुंधला सा लगता है।
सैफू.
Labels: संवाद
चाहतों से बनी जगह
जब एक दूसरे की सांस से जगह हमेशा ज़िंदा रहने का मुकाम बना लेती है तो उस जगह का दम तोड़ना या कुछ घंटों के लिए जिंदा होने की मौज़ूदगी में रहना मुश्किल हो जाता है।
उसके बीच उस जगह को कौन उस जगह के होने की मौजूदगी में रखता है, चबूतरे के मालिक को कोई लैना देना नहीं।
अब वहां कोई रात के 2 बज़े तक चाय का ठिया लगाए या अण्डे-पराठे की रेड़ी। वहां लगने वाली भीड़ उस जगह के आकर्षण के आकार को और फैलाती रहती है।
आप यहां एक दूसरे को देखकर उसके जैसा रंग अपना सकते हो, क्योंकि वो जगह ही बनी हुई है एक दूसरे के रंग से, कोई अपना रंग लेकर आता है तो कोई अपना रंग भूल किसी और के रंग में रंग जाता है। कोई अपनी जगह में रहने की हिदायत देता नज़र आता है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी करे उनका मानना है कि जैसा करेगा वैसा भुकतेगा।
हंसी-मज़ाक करते रहना और 5-10 रू के पीछे इन जगहों के हसीन पलों को छोड़ना कोई नहीं चाहता। पर ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं ये नशा है, जुआ है अपनी जिंदगी के साथ, अपने वक्त के साथ।
वो चाहते हैं कि वो समय की कदर करें और अपना समय बरबाद करने से बहतर किसी काम में लगाऐं, पर उस जगह में आ रहे लोग इन बातों से कहां प्रभावित होने वाले, वो जानते हैं तो बस...
"कुछ पल की जिंदगी है, आज है कल नहीं तो कुछ पल अपने लिए ही सही" जिसमें मैं हूँ, मेरे दोस्त हों, मेरा अंदाज़ हो, हमारी हँसी हो, एक-दूसरे का सुनना सुनाना हो, कभी सलाह मशवरा हो तो कभी-कभी बस यूंही आना हो।
पर कुछ पल हों जो अपने काम से परे हों, घर-परिवार से परे हो, करीयर की टेंशन से परे हो और उसमें हो वो जो मज़ा भी दे और खुशी भी, जिसमें बार-बार जाना कभी बोरियत न बने, बने तो बस दुबारा बार-बार जाने का नशा, रोज़ अलग मज़े का नशा।
जिसको में उस जगह के आकर्षण के रूप में देखू तो कभी ज़िद या आदत में।
यहां कौन कहां से आता है? क्या करके आता है? कब आता है? और कब तक जाता है?
ये न तो किसी को जानने की जरूरत है और न ही किसी को बताने की...
यहां बहुत कुछ अपनी मर्ज़ी पर निर्भर होता है और बहुत कुछ नहीं भी।
सैफू.
Labels: महफिलों के बीच से... , शिरकत
बनाने से बनने तक...
वहां से होकर गुज़र जाने वाले क्या समझते हैं उस जगह को, वहा बैठे लोगों को, उनकी सोच से परे ये जगह आपके सामने हमेशा वेलकम ही बोलती नज़र आती है। कभी वहां की आँखों से तो कभी वहां की बातों से...
इस जगह से कभी गालियाँ बाहर आती है तो कभी उनका बचपन या बचपना, कभी किसी का बड़ा होना बाहर आता है तो कभी किसी का सीख का गुरूर....
सबके बनने या बढ़ने का दायेरा चाहे कितना ही क्यों न हो वो निकलता है उसी गेट से जहां से वो जगह मे शामिल हुआ था।
हर कोई अपने लिए उस चार दिवारी में कुछ न कुछ तैयार ही करता मिलता और जब बाहर आता लोगों या महफिलों में उतरता तो एक पहचान, नाम या अंदाज़ मे, जिससे कभी उसे नवाज़ा भी जाता तो कभी चिड़ाया भी।
कभी वही नाम और अंदाज़ उसकी कमाई का ज़रिया बन जाता तो कभी मज़ाक की शक़्ल मे उसे खड़ा कर उसके नाम और अंदाज़ से मज़ाकिया माहौल तैयार किया जाता।
बनने वाला भी उन्ही में से कोई एक होता और बनाने वाला भी।
सैफू.