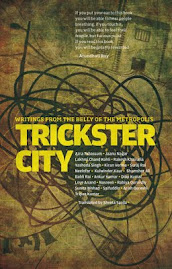दिल्ली 06 उन पहलूओं से बना हुआ है जो पल-पल हर एक नज़र में आपको एक नई भाषा देता है माहौल को बयां करने की, जिसमें टाइम-टेबल और सिमटते माहौल में भी एक-दूसरे को वो खुशी बांटते चहरें मिल जाते हैं जो इस दौर में कहीं गुम से लगते हैं।
पल-पल की कीमत होती है ये कहता है हमारा समाज, घर-परिवार, हमारा खुद पर हमारा खुद भी हमसे कुछ चाहता है और उसी चाहत में लिपटे लोग अपने खुद को महफिलों मे उतार आ मिलते हैं जिल्ली-06 की उन जगहों में जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हर जगह अपना समाज खुद तैयार करती है और दिल्ली-06 का अपना खुद का समाज है तभी इसे पुरानी ज़ुबानों से लेकर आज तक पुरानी दिल्ली ही कहा जाता है जिसमें कहने-सुनने वालों की भाषा भी वही मांगता है जो उनका खुद चाहता है।
लोगों की चाहत से जगहों का बनना पुरानी दिल्ली की ख़ासियत है। जिसमें हर एक जगह अपने होने पर गर्व करती है और वहां से निकलती आवाज़े कहती हैं "हम अपने मालिक खुद हैं, कोई ओर कौन होता है हमें रोकने वाला" जिसमें कभी बड़े-बूड़े अपनी बहकती आवाज़ में कहते नज़र आते हैं
"पुरानी दिल्ली, दिल्ली का वो कोना है, जो दिल्ली को पहचान देता है।"
"यहां जैसा बाज़ार और महफिलें ओर कहां?”
"दिल्ली बदल रही है पर पुरानी दिल्ली जो थी वो है और अल्लाह ने चाहा तो ऐसी ही रहेगी"
तो कभी घूमते चहरे, आवाज़ें लगाते बैझिझक लोग माहौल को बदलाव के भाव में उतारते से लगते हैं। जिसमें कभी चाय के ठिए शामिल हो जाते हैं तो कभी रेढ़ियों पर लगा फल-फ्रूट का मेला जो रोज़ की रोनक है। कभी ओरों की चाहत को अपनी दुकान मे सजा लोग खेंचते नज़र आते हैं लोगों को तो कभी लड़ाई झगड़ो से शांत सी दिखती गलियाँ, चौराहें और बाज़ार।
बाहर दिखता है वो जो सुनने में आता है पर इसके अंदर अपनी चाहतों के दरवाजों को कोई खोले बैठा है।
हर एक गली, हर एक मोड़ और चौराहा उसमें रहने वालों की मांग और चाहत की समझ से बनाए बैठा है वो महकमें जो टाइम-पास जैसी भाषा में अपने को वहां जमाए हुए हैं जिसमें उतरकर कई लोग जीते है, जिसमें जगह और लोग एक दूसरे की रोज़मर्रा को सजाते से लगते हैं।
कैरम क़्लब, चाय की दुकानें और ठिए, वीडियो गेम, जिम ऐसे कई महकमें अपनी अपनी परिभाषा लिए पुरानी दिल्ली मे उसी के टाइम-टेबल के अनुसार अपनी व्यवस्था और बनावट में हैं।
सैफू.
Delhi-06
इस बनने की शुरूआत कैसे हुई?
 राहों से अपनी पसन्द की चिज़ों को चुनकर इकठ्ठा करना और अपना घर तैयार करना।
राहों से अपनी पसन्द की चिज़ों को चुनकर इकठ्ठा करना और अपना घर तैयार करना।
यही तरीका है केरम क्लब के बनने का जिसमें क्लब का मालिक अपनी मर्ज़ी से क्लब को किसी तैय्यारी में सजाता है।
पसन्द न पसन्द आर्कषण के मुताबिक माहौलों को देखकर तैयार करता। जहाँ माहौल टाईम-पास होने का या करने का समय नहीं देता वहाँ केरम जैसे टाईम-पास खेलों को जगह मिल जाती है। जिसमें महफिल बनती, जुड़ती, संवर कर अपना खेल पैना करती नज़र आती है। खेल को पैना करना और उस खेल को बनाए रखने की होड़ में महफिलें इन जगहों को अपनी रोज़मर्रा में जोड़ लेती है।
एक केरम क्लब अपनी लम्बाई-चौड़ाई को जब तक लोगों की मौजूदगी से भर नहीं लेता तब तक कैरम क्लब खाली सा लगता है पर जब भीड़ होती है तो जगह का मालिक अपनी बनावटी दुनिया से खुश हो जाता है।
दो कैरम बोर्डो का यह महकमा सिमटता और अपने में सबको समेटता सा लगता है।
पर सब भूल लोग अपने हुनर को दिखाने में लग जाते हैं जिसमें से अनेक परछाईयाँ अपना प्रतिबिम्ब छोड़ चली जाती हैं। जिनकी छोड़ी गई धूल हर कोने में लगी दिखती है। वो कोना उनकी याद के साथ तैयार हो कर कुछ पलों को याद करने का रुप बन जाता है।
हर किसी के पास अपने समय का चक़्कर अपने हाथ की उंगलियों पर गढ़ा है। जिसमें से हर उंगली अपनी एक प्रतिक्रिया में मशरुफ़ नज़र आती है। जिसके खाली स्पेस में केरम जेसा खेल अपना भराव बनाए हुए है।
Labels: देखा-देखी , महफिलों के बीच से...
जगहें ...
कई जगहें हमें अपने आप मे सिमटने और बहने के बहाने देती हैं, वो बहाने जो कभी हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं तो कभी रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी एक जगह बना लेते हैं। और उनका ये जगह बनाना हमें उस पर सोचने और बोलने के कई तरीके दे जाते हैं, वो तरीके जो कभी हम दोस्तों की मण्डलियों में बोलते नज़र आते हैं तो कभी किताबों मे लिखते।
क्योंकि हर जगह पहले वक़्त मांगती है फिर आपकी आदत और फिर उसके तरीकों की एक समझ कि यहां कब, कैसे और क्यूं?
और वहीं समझ हमारे शब्दों में उस जगह के लिए एक शब्द और जोड़ देती है, कभी
वाह-वाह में तो कभी टाइम-पास में कभी मस्ती में तो कभी दोस्ती और आदत में।
जगहें अपनी समझ, अपनी बातें, अपनी अच्छाई और बुराई सब को अपने ही शब्दों में समेटे रखती है। और उसका ये समेटना जगह को बढ़ोतरी के पाएदान पर चढ़ा देता है।
क्योकि यहां आने-जाने वालों की कमी को महसूस नहीं किया जाता जिसमे बाहर से आ रहे शब्द जो बाहर के ही रहते हैं और अंदर बोले जाने वाली बोली जो सिर्फ वहीं की हैं, उस जगह को एक अलग ही जगह बना देती है।
किसी को यहां आना अच्छा लगता है तो किसी ने अपने जीवन के 10-12 साल के कई घंटे यहां दिये हैं, कोई यहां चैम्पीयन है तो कोई सिखना चाहता है, कोई रोज़ की चाय का शौकिन है तो कोई ठियों पर खड़े होकर चाय पीने को ही मज़ेदारी मानता है। सब अपनी ही धुन में है पर ये धुन सिर्फ लड़कों तक ही सीमित है अब वो चाय के ठियें हो या दुकान, कैरम क़्लब हो या वीडियो गैम की दुकान या फिर जिम....
सब अपने-अपने तरोकों से जगह से जुड़ते हैं उसे अपनाते हैं, उठते-बैठते हैं, मज़े करते हैं, खेलते हैं या खड़े होते हैं सबको अपनी जगह, मिलने वाला माहौल और आदत या शौक़ से लगाव है जो कि उस जगह से जुड़ा है।
सैफू...
बनने- बनाने के बीच में...
कुछ जगहें जो अपनी और दूसरों की संतुष्टि को पूर्ण करने की इच्छा ज़ाहिर करती रहती हैं। कुछ अनमोल ठिकाने जो बहुमूल्य कामों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। उसी में बैठे लोग अपनी खांचेदार ज़िन्दगी को जोड़ते जाते हैं, अपनी जरुरतों, कामों और महफिलों को जमाने में इच्छुक लोग घूमते, बनाते चलते हैं अपनी मनचाही जगाहों को।
यह लोग वो होते हैं जो छाल नुमा ज़िन्दगी को जीते जाते हैं और हर वाद-अपवाद को अपने शरीर से दूर कर नई छाल की बुनाई में लग जाते हैं।
फिर शुरु होती है समुह गढ़ने की एक अनुठी प्रतिक्रिया। जिसमें अवज्ञा और अनादर को दूर हटाकर अपने बनाए कस्बों मे विलीन होने की शक्ति होती हैं। वो कस्बें जो अन्नत में खत्म होते और फिर अपने प्रतिबिन्द की तरह ही बनते जाते हैं।
इसमे प्रकाश और अंधकार दोनों ही इन कस्बों को बनाने और बिगाड़ने में निपुर्ण है।
प्रकाश जो कि महफिल की रोनक में सब दिखाता है, सच हो या झूट। पर अंधकार अपनी चपेट में सब को लेकर विलीन होने की कंगार पर नज़र आता हैं।
इसमे सर्वदा अपना पाठ लिए घूम रहा हैं, जो टाईम-टेबल के हिसाब से आपको अपनी रुटीन में घूमाता रहता है। वो नवीन इच्छाओं को गाठ-व-गाठ बांधकर एक जालीदार ढ़ांचा तैयार करता है।
उसे आप ओढ़ कुछ हदतक लोगों की छायादार वाणी से बच पाते हो। मगर आप अंजान नहीं हो, क्योंकि जालीदार ढ़ांचे की वजह से आप अपने कुल में हो रहे संवाद को परखते और जोड़ते चलते हो...
...मनोज...
Labels: महफिलों के बीच से... , संवाद